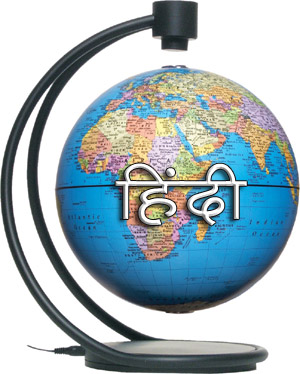सामयिकी
१
हिंदी का वैश्विक परिदृश्य
डा. करुणाशंकर उपाध्याय
इक्कीसवीं सदी बीसवीं शताब्दी से भी ज्यादा तीव्र परिवर्तनों वाली तथा चमत्कारिक उपलब्धियों वाली शताब्दी सिद्ध हो रही है। विज्ञान एवं तकनीक के सहारे पूरी दुनिया एक वैश्विक गाँव में तब्दील हो रही है और स्थलीय व भौगोलिक दूरियां अपनी अर्थवत्ता खो रहीं हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था आर्थिक और व्यापारिक आधार पर ध्रुवीकरण तथा पुनर्संघटन की प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों के महत्त्व का क्रम भी बदल रहा है।
बदलती दुनिया बदलते भाषिक परिदृष्य
यदि हम विगत तीन शताब्दियों पर विचार करें तो कई रोचक निष्कर्ष पा सकते हैं। यदि अठारहवीं सदी आस्ट्रिया और हंगरी के वर्चस्व की रही है तो उन्नीसवीं सदी ब्रिटेन और जर्मनी के वर्चस्व का साक्ष्य देती है। इसी तरह बीसवीं सदी अमेरिका एवं सोवियत संघ के वर्चस्व के रूप में विश्व नियति का निदर्शन करने वाली रही है। आज स्थिति यह है कि लगभग विश्व समुदाय दबी जुबान से ही सही, यह कहने लगा है कि इक्कीसवीं सदी भारत और चीन की होगी। इस सदी में इन दोनों देशों की तूती बोलेगी। इस भविष्यवाणी को चरितार्थ करने वाले ठोस कारण हैं। आज भारत और चीन विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं तथा विश्व स्तर पर इनकी स्वीकार्यता और महत्ता स्वत: बढ रही है। इन देशों के पास अकूत प्राकृतिक संपदा तथा युवतर मानव संसाधन है जिसके कारण ये भावी वैश्विक संरचना में उत्पादन के बडे स्रोत बन सकते हैं। अपनी कार्य निपुणता तथा निवेश एवं उत्पादन के समीकरण की प्रबल संभावना को देखते हुए ही भारत और चीन को निकट भविष्य की विश्व शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है।
जाहिर है कि जब किसी राष्ट्र को विश्व बिरादरी अपेक्षाकृत ज्यादा महत्त्व और स्वीकृति देती है तथा उसके प्रति अपनी निर्भरता में इजाफा पाती है तो उस राष्ट्र की तमाम चीजें स्वत: महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में भारत की विकासमान अंतरराष्ट्रीय हैसियत हिंदी के लिए वरदान-सदृश है। यह सच है कि वर्तमान वैश्विक परिवेश में भारत की बढती उपस्थिति हिंदी की हैसियत का भी उन्नयन कर रही है। आज हिंदी राष्ट्रभाषा की गंगा से विश्वभाषा का गंगासागर बनने की प्रक्रिया में है।
भाषा के वैश्विक संदर्भ की विशेषताएँ-
आखिर, वे कौन सी विशेषताएँ हैं जो किसी भाषा को वैश्विक संदर्भ प्रदान करती हैं। ऐसा करके हम हिंदी के विश्व संदर्भ का वस्तुपरक विश्लेषण कर सकते हैं। जब हम हिंदी को विश्व भाषा में रूपांतरित होते हुए देख रहे हैं और यथावसर उसे विश्वभाषा की संज्ञा प्रदान कर रहे हैं, तब यह जरूरी हो जाता है कि हम सर्वप्रथम विश्वभाषा का स्वरूप विश्लेषण कर लें। संक्षेप में विश्वभाषा के निम्नलिखित लक्षण निर्मित किए जा सकते हैं:-
-
उसके बोलने-जानने तथा चाहने वाले भारी तादाद में हों और वे विश्व के अनेक देशों में फैले हों।
-
उस भाषा में साहित्य-सृजन की प्रदीर्घ परंपरा हो और प्राय: सभी विधाएँ वैविध्यपूर्ण एवं समृद्ध हों। उस भाषा में सृजित कम-से-कम एक विधा का साहित्य विश्वस्तरीय हो।
-
उसकी शब्द-संपदा विपुल एवं विराट हो तथा वह विश्व की अन्यान्य बडी भाषाओं से विचार-विनिमय करते हुए एक -दूसरे को प्रेरित -प्रभावित करने में सक्षम हो।
-
उसकी शाब्दी एवं आर्थी संरचना तथा लिपि सरल, सुबोध एवं वैज्ञानिक हो। उसका पठन-पाठन और लेखन सहज-संभाव्य हो। उसमें निरंतर परिष्कार और परिवर्तन की गुंजाइश हो।
-
उसमें ज्ञान-विज्ञान के तमाम अनुशासनों में वाङमय सृजित एवं प्रकाशित हो तथा नए विषयों पर सामग्री तैयार करने की क्षमता हो।
-
वह नवीनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों के साथ अपने-आपको पुरस्कृत एवं समायोजित करने की क्षमता से युक्त हो।
-
वह अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भों, सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक चिंताओं तथा आर्थिक विनिमय की संवाहक हो।
-
वह जनसंचार माध्यमों में बडे पैमाने पर देश-विदेश में प्रयुक्त हो रही हो।
-
उसका साहित्य अनुवाद के माध्यम से विश्व की दूसरी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में पहुँच रहा हो।
-
उसमें मानवीय और यांत्रिक अनुवाद की आधारभूत तथा विकसित सुविधा हो जिससे वह बहुभाषिक कम्प्यूटर की दुनिया में अपने समग्र सूचना स्रोत तथा प्रक्रिया सामग्री (सॉफ्टवेयर) के साथ उपलब्ध हो। साथ ही, वह इतनी समर्थ हो कि वर्तमान प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों मसलन ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-बुक, इंटरनेट तथा एस.एम.एस. एवं वेब जगत में प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी सक्रिय उपस्थिति का अहसास करा सके ।
-
उसमें उच्चकोटि की पारिभाषिक शब्दावली हो तथा वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीनतम आविष्कृतियों को अभिव्यक्त करते हुए मनुष्य की बदलती जरूरतों एवं आकांक्षाओं को वाणी देने में समर्थ हो।
-
वह विश्व चेतना की संवाहिका हो। वह स्थानीय आग्रहों से मुक्त विश्व दृष्टि सम्पन्न कृतिकारों की भाषा हो, जो विश्वस्तरीय समस्याओं की समझ और उसके निराकरण का मार्ग जानते हों।
वैश्विक संदर्भ में हिंदी की सामर्थ्य
जब हम उपर्युक्त प्रतिमानों पर हिंदी का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि वह न्यूनाधिक मात्रा में प्राय: सभी निष्कर्षों पर खरी उतरती है। आज वह विश्व के सभी महाद्वीपों तथा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों- जिनकी संख्या लगभग एक सौ चालीस है- में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त होती है। वह विश्व के विराट फलक पर नवल चित्र के समान प्रकट हो रही है। आज वह बोलने वालों की संख्या के आधार पर चीनी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बडी भाषा बन गई है। इस बात को सर्वप्रथम सन १९९९ में "मशीन ट्रांसलेशन समिट' अर्थात् यांत्रिक अनुवाद नामक संगोष्ठी में टोकियो विश्वविद्यालय के प्रो. होजुमि तनाका ने भाषाई आँकडे पेश करके सिद्ध किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आँकडों के अनुसार विश्वभर में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय है। अंग्रेजी तो तीसरे क्रमांक पर पहुँच गई है। इसी क्रम में कुछ ऐसे विद्वान अनुसंधित्सु भी सक्रिय हैं जो हिंदी को चीनी के ऊपर अर्थात् प्रथम क्रमांक पर दिखाने के लिए प्रयत्नशील हैं। डॉ. जयन्ती प्रसाद नौटियाल ने भाषा शोध अध्ययन २००५ के हवाले से लिखा है कि, विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या एक अरब दो करोड पच्चीस लाख दस हजार तीन सौ बावन (१, ०२, २५, १०,३५२) है जबकि चीनी बोलने वालों की संख्या केवल नब्बे करोड चार लाख छह हजार छह सौ चौदह (९०, ०४,०६,६१४) है। यदि यह मान भी लिया जाय कि आँकडे झूठ बोलते हैं और उन पर आँख मूँदकर विश्वास नहीं किया जा सकता तो भी इतनी सच्चाई निर्विवाद है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर विश्व की दो सबसे बडी भाषाओं में से है। लेकिन वैज्ञानिकता का तकाजा यह भी है कि हम इस तथ्य को भी स्वीकार करें कि अंग्रेजी के प्रयोक्ता विश्व के सबसे ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा वैचारिक गतिविधियों को चलाने वाली सबसे प्रभावशाली भाषा बनी हुई है। चूंकि हिंदी का संवेदनात्मक साहित्य उच्चकोटि का होते हुए भी ज्ञान का साहित्य अंग्रेजी के स्तर का नहीं है अत: निकट भविष्य में विश्व व्यवस्था परिचालन की दृष्टि से अंग्रेजी की उपादेयता एवं महत्त्व को कोई खतरा नहीं है। इस मोर्चे पर हिंदी का बडे ही सबल तरीके से उन्नयन करना होगा। उसके पक्ष में महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आज अंग्रेजी के बाद वह विश्व के सबसे ज्यादा देशों में व्यवहृत होती है।
आने वाली पीढ़ी की भाषा-
वर्तमान उत्तर आधुनिक परिवेश में विशाल जनसंख्या भारत और चीन के साथ-साथ हिंदी और चीनी के लिए भी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। हमारे देश में १९८० के बाद ६५ करोड से ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं। जो विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षित प्रशिक्षित हो रहे हैं। वे सन् २०२५ तक विधिवत प्रशिक्षित पेशेवर के रूप में अपनी सेवाएँ देने के लिए विश्व के समक्ष उपलब्ध होंगे। दूसरी ओर जापान की साठ प्रतिशत से ज्यादा आबादी साठ साल पार करके बुढापे की ओर बढ रही है। यही हाल आगामी पंद्रह सालों में अमेरिका और यूरोप का भी होने वाला है । ऐसी स्थिति में विश्व का सबसे तरुण मानव संसाधन होने के कारण भारतीय पेशेवरों की तमाम देशों में लगातार मांग बढेगी। जाहिर है कि जब भारतीय पेशेवर भारी तादाद में दूसरे देशों में जाकर उत्पादन के स्रोत बनेंगे। वहाँ की व्यवस्था परिचालन का सशक्त पहिया बनेंगे तब उनके साथ हिंदी भी जाएगी। ऐसी स्थिति में जहाँ भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में होगा वहाँ हिंदी स्वत: विश्वमंच पर प्रभावी भूमिका का वहन करेगी। इस तरह यह माना जा सकता है कि हिंदी आज जिस दायित्व बोध को लेकर संकल्पित है वह निकट भविष्य में उसे और भी बडी भूमिका का निर्वाह करने का अवसर प्रदान करेगा। हिंदी जिस गति तथा आंतरिक ऊर्जा के साथ अग्रसर है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि सन २०२० तक वह दुनिया की सबसे ज्यादा बोली व समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी।
समर्थ भाषा और वैज्ञानिक लिपि-
यदि हम इन आँकडों पर विश्वास करें तो संख्याबल के आधार पर हिंदी विश्वभाषा है। हाँ, यह जरूर संभव है कि यह मातृभाषा न होकर दूसरी, तीसरी अथवा चौथी भाषा भी हो सकती है। हिंदी में साहित्य-सृजन की परंपरा भी बारह सौ साल पुरानी है। वह ८वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान २१वीं शताब्दी तक गंगा की अनाहत-अविरल धारा की भाँति प्रवाहमान है। उसका काव्य साहित्य तो संस्कृत के बाद विश्व के श्रेष्ठतम साहित्य की क्षमता रखता है। उसमें लिखित उपन्यास एवं समालोचना भी विश्वस्तरीय है। उसकी शब्द संपदा विपुल है। उसके पास पच्चीस लाख से ज्यादा शब्दों की सेना है। उसके पास विश्व की सबसे बडी कृषि विषयक शब्दावली है। उसने अन्यान्य भाषाओं के बहुप्रयुक्त शब्दों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया है और जो शब्द अप्रचलित अथवा बदलते जीवन संदर्भों से दूर हो गए हैं उनका त्याग भी कर दिया है। आज हिंदी में विश्व का महत्त्वपूर्ण साहित्य अनुसृजनात्मक लेखन के रूप में उपलब्ध है और उसके साहित्य का उत्तमांश भी विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जा रहा है।
जहाँ तक देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का सवाल है तो वह सर्वमान्य है। देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएँ उच्चारण पर आधारित हैं। हिंदी की शाब्दी और आर्थी संरचना प्रयुक्तियों के आधार पर सरल व जटिल दोनों है। हिंदी भाषा का अन्यतम वैशिष्ट्य यह है कि उसमें संस्कृत के उपसर्ग तथा प्रत्ययों के आधार पर शब्द बनाने की अभूतपूर्व क्षमता है। हिंदी और देवनागरी दोनों ही पिछले कुछ दशकों में परिमार्जन व मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजरी हैं जिससे उनकी संरचनात्मक जटिलता कम हुई है। हम जानते हैं कि विश्व मानव की बदलती चिंतनात्मकता तथा नवीन जीवन स्थितियों को व्यंजित करने की भरपूर क्षमता हिंदी भाषा में है बशर्ते इस दिशा में अपेक्षित बौद्धिक तैयारी तथा सुनियोजित विशेषज्ञता हासिल की जाए। आखिर, उपग्रह चैनल हिंदी में प्रसारित कार्यक्रमों के जरिए यही कर रहे हैं।
मीडिया और वेब पर हिंदी-
यह सत्य है कि हिंदी में अंग्रेजी के स्तर की विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित पुस्तकें नहीं हैं। उसमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों पर उच्चस्तरीय सामग्री की दरकार है। विगत कुछ वर्षों से इस दिशा में उचित प्रयास हो रहे हैं। अभी हाल ही में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हिंदी माध्यम में एम.बी.ए.का पाठ¬क्रम आरंभ किया गया। इसी तरह "इकोनामिक टाइम्स' तथा "बिजनेस स्टैंडर्ड' जैसे अखबार हिंदी में प्रकाशित होकर उसमें निहित संभावनाओं का उद्घोष कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों में यह भी देखने में आया कि "स्टार न्यूज' जैसे चैनल जो अंग्रेजी में आरंभ हुए थे वे विशुद्ध बाजारीय दबाव के चलते पूर्णत: हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए। साथ ही, "ई.एस.पी.एन' तथा "स्टार स्पोर्ट्स' जैसे खेल चैनल भी हिंदी में कमेंट्री देने लगे हैं। हिंदी को वैश्विक संदर्भ देने में उपग्रह-चैनलों, विज्ञापन एजेंसियों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा यांत्रिक सुविधाओं का विशेष योगदान है। वह जनसंचार-माध्यमों की सबसे प्रिय एवं अनुकूल भाषा बनकर निखरी है।
आज विश्व में सबसे ज्यादा पढे जानेवाले समाचार पत्रों में आधे से अधिक हिन्दी के हैं। इसका आशय यही है कि पढा-लिखा वर्ग भी हिन्दी के महत्त्व को समझ रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि आज भारतीय उपमहाद्वीप ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, मॉरीशस,चीन,जापान,कोरिया, मध्य एशिया, खाडी देशों, अफ्रीका, यूरोप, कनाडा तथा अमेरिका तक हिंदी कार्यक्रम उपग्रह चैनलों के जरिए प्रसारित हो रहे हैं और भारी तादाद में उन्हें दर्शक भी मिल रहे हैं। आज मॉरीशस में हिंदी सात चैनलों के माध्यम से धूम मचाए हुए है। विगत कुछ वर्षों में एफ.एम. रेडियो के विकास से हिंदी कार्यक्रमों का नया श्रोता वर्ग पैदा हो गया है। हिंदी अब नई प्रौद्योगिकी के रथ पर आरूढ होकर विश्वव्यापी बन रही है। उसे ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-बुक, इंटरनेट, एस.एम.एस. एवं वेब जगत में बडी सहजता से पाया जा सकता है। इंटरनेट जैसे वैश्विक माध्यम के कारण हिंदी के अखबार एवं पत्रिकाएँ दूसरे देशों में भी विविध साइट्स पर उपलब्ध हैं।
माइक्रोसाफ्ट, गूगल, सन, याहू, आईबीएम तथा ओरेकल जैसी विश्वस्तरीय कंपनियाँ अत्यंत व्यापक बाजार और भारी मुनाफे को देखते हुए हिंदी प्रयोग को बढावा दे रही हैं। संक्षेप में, यह स्थापित सत्य है कि अंग्रेजी के दबाव के बावजूद हिंदी बहुत ही तीव्र गति से विश्वमन के सुख-दु:ख, आशा-आकांक्षा की संवाहक बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व के दर्जनों देशों में हिंदी की पत्रिकाएँ निकल रही हैं तथा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, आस्ट्रिया जैसे विकसित देशों में हिंदी के कृति रचनाकार अपनी सृजनात्मकता द्वारा उदारतापूर्वक विश्व मन का संस्पर्श कर रहे हैं। हिंदी के शब्दकोश तथा विश्वकोश निर्मित करने में भी विदेशी विद्वान सहायता कर रहे हैं।
राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में हिंदी
जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विनिमय के क्षेत्र में हिंदी के अनुप्रयोग का सवाल है तो यह देखने में आया है कि हमारे देश के नेताओं ने समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में भाषण देकर उसकी उपयोगिता का उद्घोष किया है। यदि अटल बिहारी वाजपेयी तथा पी.वी.नरसिंहराव द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में दिया गया वक्तव्य स्मरणीय है तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्र मंडल देशों की बैठक तथा चन्द्रशेखर द्वारा दक्षेस शिखर सम्मेलन के अवसर पर हिंदी में दिए गए भाषण भी उल्लेखनीय हैं। यह भी सर्वविदित है कि यूनेस्को के बहुत सारे कार्य हिंदी में सम्पन्न होते हैं। इसके अलावा अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरीशस, त्रिनिदाद, लंदन, सुरीनाम तथा न्यूयार्क जैसे स्थलों पर सम्पन्न हो चुके हैं जिनके माध्यम से विश्व स्तर पर हिंदी का स्वर सम्भार महसूस किया गया। अभी आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव बान की मून ने दो-चार वाक्य हिंदी में बोलकर उपस्थित विश्व हिंदी समुदाय की खूब वाह-वाही लूटी। हिंदी को वैश्विक संदर्भ और व्याप्ति प्रदान करने में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेशों में स्थापित भारतीय विद्यापीठों की केन्द्रीय भूमिका रही है जो विश्व के अनेक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों में फैली हुई है। इन विश्वविद्यालयों में शोध स्तर पर हिन्दी अध्ययन अध्यापन की सुविधा है जिसका सर्वाधिक लाभ विदेशी अध्येताओं को मिल रहा है।
विदेशो में हिंदी-
हिंदी विश्व के प्राय: सभी महत्त्वपूर्ण देशों के विश्व विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन में भागीदार है। अकेले अमेरिका में ही लगभग एक सौ पचास से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन-पाठन हो रहा है। आज जब २१वीं सदी में वैश्वीकरण के दबावों के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ आदान -प्रदान व संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं तो हिंदी इस दिशा में विश्व मनुष्यता को निकट लाने के लिए सेतु का कार्य कर सकती है। उसके पास पहले से ही बहु सांस्कृतिक परिवेश में सक्रिय रहने का अनुभव है जिससे वह अपेक्षाकृत ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभाने की स्थिति में है। हिंदी सिनेमा अपने संवादों एवं गीतों के कारण विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुए हैं। उसने सदा-सर्वदा से विश्वमन को जोडा है। हिंदी की मूल प्रकृति लोकतांत्रिक तथा रागात्मक संबंध निर्मित करने की रही है। वह विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र की ही राष्ट्र भाषा नहीं है बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरीशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सुरीनाम जैसे देशों की सम्पर्क भाषा भी है। वह भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच खाडी देशों, मध्य एशियाई देशों, रूस, समूचे यूरोप, कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको जैसे प्रभावशाली देशों में रागात्मक जुडाव तथा विचार-विनिमय का सबल माध्यम है।
यदि निकट भविष्य में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्मित होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिक ढंग से विस्तार करते हुए भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है तो वह यथाशीघ्र इस शीर्ष विश्व संस्था की भाषा बन जाएगी। यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी वह बहुत शीघ्र वहाँ पहुँचेगी। वर्तमान समय भारत और हिंदी के तीव्र एवं सर्वोन्मुखी विकास का द्योतन कर रहा है और हम सब से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं वहाँ ईमानदारी से हिंदी और देश के विकास में हाथ बँटाएँ। सारांश यह कि हिंदी विश्व भाषा बनने की दिशा में उत्तरोत्तर अग्रसर है।
गुण और परिमाण में समृद्ध भाषा
आज स्थिति यह है कि गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से हिंदी का काव्य साहित्य अपने वैविध्य एवं बहुस्तरीयता में संपूर्ण विश्व में संस्कृत काव्य को छोड कर सर्वोपरि है। "पद्मावत', "रामचरित मानस' तथा "कामायनी' जैसे महाकाव्य विश्व की किसी भी भाषा में नहीं है। वर्तमान समय में हिंदी का कथा साहित्य भी फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी के लगभग समकक्ष है। हाँ, इतना जरूर है कि जयशंकर प्रसाद को छोड कर हिंदी के पास विश्वस्तरीय नाटककार नहीं हैं। इसकी क्षतिपूर्ति हिंदी सिनेमा द्वारा भलीभाँति होती है। वह देश की सभ्यता, संस्कृति तथा बदलते संदर्भों एवं अभिरुचियों की अभिव्यक्ति का बडा ही सफल माध्यम रहा है। आज हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में जितने रचनाकार सृजन कर रहे हैं उतने बहुत सारी भाषाओं के बोलने वाले भी नहीं हैं। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दो सौ से अधिक हिंदी साहित्यकार सक्रिय हैं जिनकी पुस्तकें छप चुकी हैं। यदि अमेरिका से "विश्वा', हिंदी जगत तथा श्रेष्ठतम वैज्ञानिक पत्रिका "विज्ञान प्रकाश' हिंदी की दीपशिखा को जलाए हुए हैं तो मॉरीशस से विश्व हिंदी समाचार, सौरभ, वसंत जैसी पत्रिकाएँ हिंदी के सार्वभौम विस्तार को प्रामाणिकता प्रदान कर रही हैं। संयुक्त अरब इमारात से वेब पर प्रकाशित होने वाले हिंदी पत्रिकाएँ अभिव्यक्ति और अनुभूति पिछले ग्यारह से भी अधिक वर्षों से लोकमानस को तृप्त कर रही हैं और दिन पर दिन इनके पाठकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।
आज जरूरत इस बात की है कि हम विधि, विज्ञान, वाणिज्य तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाठ¬सामग्री उपलब्ध कराने में तेजी लाएँ। इसके लिए समवेत प्रयास की जरूरत है। यह तभी संभव है जब लोग अपने दायित्वबोध को गहराइयों तक महसूस करें और सुदृढ़ इच्छाशक्ति के साथ संकल्पित हों। आज समय की माँग है कि हम सब मिलकर हिंदी के विकास की यात्रा में शामिल हों ताकि तमाम निकषों एवं प्रतिमानों पर कसे जाने के लिये हिंदी को सही मायने में विश्व भाषा की गरिमा प्रदान कर सकें।
साभार : अभिव्यक्ति.