अभियंता दिवस (१५ सितंबर) पर विशेष रचना:
हम अभियंता...

संजीव 'सलिल'
*
हम अभियंता!, हम अभियंता!!
मानवता के भाग्य-नियंता...

माटी से मूरत गढ़ते हैं,
कंकर को शंकर करते हैं.
वामन से संकल्पित पग धर,
हिमगिरि को बौना करते हैं.

नियति-नटी के शिलालेख पर
अदिख लिखा जो वह पढ़ते हैं.
असफलता का फ्रेम बनाकर,
चित्र सफलता का मढ़ते हैं.
श्रम-कोशिश दो हाथ हमारे-
फिर भविष्य की क्यों हो चिंता...
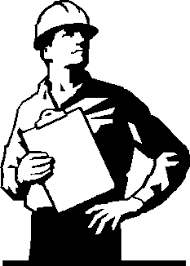
अनिल, अनल, भू, सलिल, गगन हम,
पंचतत्व औजार हमारे.
राष्ट्र, विश्व, मानव-उन्नति हित,
तन, मन, शक्ति, समय, धन वारे.

वर्तमान, गत-आगत नत है,
तकनीकों ने रूप निखारे.
निराकार साकार हो रहे,
अपने सपने सतत सँवारे.
साथ हमारे रहना चाहे,
भू पर उतर स्वयं भगवंता...

भवन, सड़क, पुल, यंत्र बनाते,
ऊसर में फसलें उपजाते.
हमीं विश्वकर्मा विधि-वंशज.
मंगल पर पद-चिन्ह बनाते.

प्रकृति-पुत्र हैं, नियति-नटी की,
आँखों से हम आँख मिलाते.
हरि सम हर हर आपद-विपदा,
गरल पचा अमृत बरसाते.
'सलिल' स्नेह नर्मदा निनादित,
ऊर्जा-पुंज अनादि-अनंता...
.

अभियंता दिवस पर मुक्तक:
*
कर्म है पूजा न भूल,
धर्म है कर साफ़ धूल।
मन अमन पायेगा तब-
जब लुटा तू आप फूल।
*
हाथ मिला, कदम उठा काम करें
लक्ष्य वरें, चलो 'सलिल' नाम करें
रख विवेक शांत रहे काम कर
श्रेष्ठ बना देश,चलो नाम करें.
*
मना अभियंता दिवस मत चुप रहो,
उपेक्षित अभियांत्रिकी है कुछ कहो।
है बहुत बदहाल शिक्षा, नौकरी-
बदल दो हालात, दुर्दशा न सहो।
*
समारोह है
*
समारोह है
सभागार में।
*
ख़ास-ख़ास आसंदी पर हैं,
खासुलखास मंच पर बैठे।
आयोजक-संचालक गर्वित-
ज्यों कौओं में बगुले ऐंठे।
करतल ध्वनि,
चित्रों-खबरों में
रूचि सबकी है
निज प्रचार में।
*
कुशल-निपुण अभियंता आए,
छाती ताने, शीश उठाए।
गुणवत्ता बिन कार्य हो रहे,
इन्हें न मतलब, आँख चुराए।
नीति-दिशा क्या सरकारों की?
क्या हो?, बात न
है विचार में।
*
मस्ती-मौज इष्ट है यारों,
चुनौतियों से भागो प्यारों।
पाया-भोगो, हँसो-हँसाओ-
वंचित को बिसराओ, हारो।
जो होता है, वह होने दो।
तनिक न रूचि
रखना सुधार में।
***
नवगीत:
उपयंत्री की यंत्रणा
संजीव
.
'अगले जनम
उपयंत्री न कीजो'
करे प्रार्थना उपअभियंता
पिघले-प्रगटे भाग्यनियंता
'वत्स! बताओ, मुश्किल क्या है?
क्यों है इस माथे पर चिंता?'
'देव! प्रमोशन एक दिला दो
फिर चाहे जो काम करा लो'
'वत्स न यह संभव हो सकता
कलियुग में सच कभी न फलता'
तेरा हर अफसर स्नातक
तुझ पर डिप्लोमा का पातक
वह डिग्री के साथ रहेगा
तुझ पर हरदम वार करेगा
तुझे भेज साईट पर सोये
तू उन्नति के अवसर खोये
तू है नींव कलश है अफसर
इसीलिये वह पाता अवसर
जे ई से ई इन सी होता
तू अपनी किस्मत को रोता
तू नियुक्त होता उपयंत्री
और रिटायर हो उपयंत्री
तेरी मेहनत उसका परचम
उसको खुशियाँ, तुझको मातम
सर्वे कर प्राक्कलन बनाता
वह स्वीकृत कर नाम कमाता
तू साईट पर बहा पसीना
वह कहलाता रहा नगीना
काम करा तू देयक लाता
वह पारित कर दाम कमाता
ठेकेदार सगे हैं उसके
पत्रकार फल पाते मिलके
मंत्री-सचिव उसी के संग हैं
पग-पग पर तू होता तंग है
पार न तू इनसे पायेगा
रोग पाल, घुट मर जाएगा
अफसर से मत, कभी होड़ ले
भूल पदोन्नति, हाथ जोड़ ले
तेरा होना नहीं प्रमोशन
तेरा होगा नहीं डिमोशन
तू मृत्युंजय, नहीं झोल दे
उठकर इनकी पोल खोल दे
खुश रह जैसा और जहाँ है
तुझसे बेहतर कौन-कहाँ है?
पाप कट रहे तेरे सारे
अफसर को ठेंगा दिखला रे!
बच्चे पढ़ें-बढ़ेंगे तेरे
तब संवरेंगे सांझ-सवेरे
अफसर सचिवालय जाएगा
बाबू बनकर पछतायेगा
कर्म योग तेरी किस्मत में
भोग-रोग उनकी किस्मत में
कह न किसी से कभी पसीजो
श्रम-सीकर में खुश रह भीजो
…
सलिल.संजीव@जीमेल.कॉम
http://divyanarmada.blogspot.com
http://hindihindi.in
हम अभियंता...
संजीव 'सलिल'
*
हम अभियंता!, हम अभियंता!!
मानवता के भाग्य-नियंता...
माटी से मूरत गढ़ते हैं,
कंकर को शंकर करते हैं.
वामन से संकल्पित पग धर,
हिमगिरि को बौना करते हैं.
नियति-नटी के शिलालेख पर
अदिख लिखा जो वह पढ़ते हैं.
असफलता का फ्रेम बनाकर,
चित्र सफलता का मढ़ते हैं.
श्रम-कोशिश दो हाथ हमारे-
फिर भविष्य की क्यों हो चिंता...
अनिल, अनल, भू, सलिल, गगन हम,
पंचतत्व औजार हमारे.
राष्ट्र, विश्व, मानव-उन्नति हित,
तन, मन, शक्ति, समय, धन वारे.
वर्तमान, गत-आगत नत है,
तकनीकों ने रूप निखारे.
निराकार साकार हो रहे,
अपने सपने सतत सँवारे.
साथ हमारे रहना चाहे,
भू पर उतर स्वयं भगवंता...
भवन, सड़क, पुल, यंत्र बनाते,
ऊसर में फसलें उपजाते.
हमीं विश्वकर्मा विधि-वंशज.
मंगल पर पद-चिन्ह बनाते.
प्रकृति-पुत्र हैं, नियति-नटी की,
आँखों से हम आँख मिलाते.
हरि सम हर हर आपद-विपदा,
गरल पचा अमृत बरसाते.
'सलिल' स्नेह नर्मदा निनादित,
ऊर्जा-पुंज अनादि-अनंता...
.
अभियांत्रिकी
*
(हरिगीतिका छंद विधान: १ १ २ १ २ x ४, पदांत लघु गुरु, चौकल पर जगण निषिद्ध, तुक दो-दो चरणों पर, यति १६-१२ या १४-१४ या ७-७-७-७ पर)
*
कण जोड़ती, तृण तोड़ती, पथ मोड़ती, अभियांत्रिकी
बढ़ती चले, चढ़ती चले, गढ़ती चले, अभियांत्रिकी
उगती रहे, पलती रहे, खिलती रहे, अभियांत्रिकी
रचती रहे, बसती रहे, सजती रहे, अभियांत्रिकी
*
नव रीत भी, नव गीत भी, संगीत भी, तकनीक है
कुछ हार है, कुछ प्यार है, कुछ जीत भी, तकनीक है
गणना नयी, रचना नयी, अव्यतीत भी, तकनीक है
श्रम मंत्र है, नव यंत्र है, सुपुनीत भी तकनीक है
*
यह देश भारत वर्ष है, इस पर हमें अभिमान है
कर दें सभी मिल देश का, निर्माण यह अभियान है
गुणयुक्त हों अभियांत्रिकी, श्रम-कोशिशों का गान है
परियोजना त्रुटिमुक्त हो, दुनिया कहे प्रतिमान है
*
तक रहा तकनीक को यदि आम जन कुछ सोचिए।
तज रहा निज लीक को यदि ख़ास जन कुछ सोचिए।।
हो रहे संपन्न कुछ तो यह नहीं उन्नति हुई-
आखिरी जन को मिला क्या?, निकष है यह सोचिए।।
*
चेन ने डोमेन की, अब मैन को बंदी किया।
पिया को ऐसा नशा ज्यों जाम साकी से पिया।।
कल बना, कल गँवा, कलकल में घिरा खुद आदमी-
किया जाए किस तरह?, यह ही न जाने है जिया।।
*
किस तरह स्मार्ट हो सिटी?, आर्ट है विज्ञान भी।
यांत्रिकी तकनीक है यह, गणित है, अनुमान भी।।
कल्पना की अल्पना सज्जित प्रगति का द्वार हो-
वास्तविकता बने ऐपन तभी जन-उद्धार हो।।
***
तज रहा निज लीक को यदि ख़ास जन कुछ सोचिए।।
हो रहे संपन्न कुछ तो यह नहीं उन्नति हुई-
आखिरी जन को मिला क्या?, निकष है यह सोचिए।।
*
चेन ने डोमेन की, अब मैन को बंदी किया।
पिया को ऐसा नशा ज्यों जाम साकी से पिया।।
कल बना, कल गँवा, कलकल में घिरा खुद आदमी-
किया जाए किस तरह?, यह ही न जाने है जिया।।
*
किस तरह स्मार्ट हो सिटी?, आर्ट है विज्ञान भी।
यांत्रिकी तकनीक है यह, गणित है, अनुमान भी।।
कल्पना की अल्पना सज्जित प्रगति का द्वार हो-
वास्तविकता बने ऐपन तभी जन-उद्धार हो।।
***
*
कर्म है पूजा न भूल,
धर्म है कर साफ़ धूल।
मन अमन पायेगा तब-
जब लुटा तू आप फूल।
*
हाथ मिला, कदम उठा काम करें
लक्ष्य वरें, चलो 'सलिल' नाम करें
रख विवेक शांत रहे काम कर
श्रेष्ठ बना देश,चलो नाम करें.
*
मना अभियंता दिवस मत चुप रहो,
उपेक्षित अभियांत्रिकी है कुछ कहो।
है बहुत बदहाल शिक्षा, नौकरी-
बदल दो हालात, दुर्दशा न सहो।
*
सोरठा सलिला:
हो न यंत्र का दास
संजीव
*
*
हो न यंत्र का दास, मानव बने समर्थ अब
रख खुद पर विश्वास, 'सलिल' यांत्रिकी हो सफल
*
*
गुणवत्ता से आप, करिए समझौता नहीं
रहे सजगता व्याप, श्रेष्ठ तभी निर्माण हो
*
*
भूलें नहीं उसूल, कालजयी निर्माण हों
कर त्रुटियाँ उन्मूल, यंत्री नव तकनीक चुन
*
कर त्रुटियाँ उन्मूल, यंत्री नव तकनीक चुन
*
निज भाषा में पाठ, पढ़ो- कठिन भी हो सरल
होगा तब ही ठाठ, हिंदी जगवाणी बने
*
*
ईश्वर को दें दोष, ज्यों बिन सोचे आप हम
पाते हैं संतोष, त्यों यंत्री को कोसकर
*
*
जब समाज हो भ्रष्ट, कैसे अभियंता करे
कार्य न हों जो नष्ट, बचा रहे ईमान भी
*
करें कल्पना आप, करिए उनको मूर्त भी
समय न सकता नाप, यंत्री के अवदान को
*
*
उल्लाला सलिला:
संजीव
*
*
(छंद विधान १३-१३, १३-१३, चरणान्त में यति, सम चरण सम तुकांत, पदांत एक गुरु या दो लघु)
*
*
अभियंता निज सृष्टि रच, धारण करें तटस्थता।
भोग करें सब अनवरत, कैसी है भवितव्यता।।
*
*
मुँह न मोड़ते फ़र्ज़ से, करें कर्म की साधना।
जगत देखता है नहीं, अभियंता की भावना।।
*
*
सूर सदृश शासन मुआ, करता अनदेखी सतत।
अभियंता योगी सदृश, कर्म करें निज अनवरत।।
*
*
भोगवाद हो गया है, सब जनगण को साध्य जब।
यंत्री कैसे हरिश्चंद्र, हो जी सकता कहें अब??
*
*
भृत्यों पर छापा पड़े, मिलें करोड़ों रुपये तो।
कुछ हजार वेतन मिले, अभियंता को क्यों कहें?
*
नेता अफसर प्रेस भी, सदा भयादोहन करें।
गुंडे ठेकेदार तो, अभियंता क्यों ना डरें??
*
समझौता जो ना करे, उसे तंग कर मारते।
यह कड़वी सच्चाई है, सरे आम दुत्कारते।।
*
हर अभियंता विवश हो, समझौते कर रहा है।
बुरे काम का दाम दे, बिन मारे मर रहा है।।
*
मिले निलम्बन-ट्रान्सफर, सख्ती से ले काम तो।
कोई न यंत्री का सगा, दोषारोपण सब करें।।
*
कुछ हजार वेतन मिले, अभियंता को क्यों कहें?
*
नेता अफसर प्रेस भी, सदा भयादोहन करें।
गुंडे ठेकेदार तो, अभियंता क्यों ना डरें??
*
समझौता जो ना करे, उसे तंग कर मारते।
यह कड़वी सच्चाई है, सरे आम दुत्कारते।।
*
हर अभियंता विवश हो, समझौते कर रहा है।
बुरे काम का दाम दे, बिन मारे मर रहा है।।
*
मिले निलम्बन-ट्रान्सफर, सख्ती से ले काम तो।
कोई न यंत्री का सगा, दोषारोपण सब करें।।
*
हम हैं अभियंता
संजीव
*
*
(छंद विधान: १० ८ ८ ६ = ३२ x ४)
*
*
हम हैं अभियंता नीति नियंता, अपना देश सँवारेंगे
हर संकट हर हर मंज़िल वरकर, सबका भाग्य निखारेंगे
पथ की बाधाएँ दूर हटाएँ, खुद को सब पर वारेंगे
भारत माँ पावन जन-मन भावन, सीकर चरण पखारेंगे
*
*
अभियंता मिलकर आगे चलकर, पथ दिखलायें जग देखे
कंकर को शंकर कर दें हँसकर मंज़िल पाएं कर लेखे
शशि-मंगल छूलें, धरा न भूलें, दर्द दीन का हरना है
आँसू न बहायें , जन यश गाये, पंथ वही नव वरना है
*
*
श्रम-स्वेद बहाकर, लगन लगाकर, स्वप्न सभी साकार करें
गणना कर परखें, पुनि-पुनि निरखें, त्रुटि न तनिक भी कहीं वरें
उपकरण जुटायें, यंत्र बनायें, नव तकनीक चुनें न रुकें
आधुनिक प्रविधियाँ, मनहर छवियाँ, उन्नत देश करें न चुकें
*
*
नव कथा लिखेंगे, पग न थकेंगे, हाथ करेंगे काम सदा
किस्मत बदलेंगे, नभ छू लेंगे, पर न कहेंगे 'यही बदा'
प्रभु भू पर आयें, हाथ बटायें, अभियंता संग-साथ रहें
श्रम की जयगाथा, उन्नत माथा, सत नारायण कथा कहें
श्रम की जयगाथा, उन्नत माथा, सत नारायण कथा कहें
================================
एक रचना:समारोह है
*
समारोह है
सभागार में।
*
ख़ास-ख़ास आसंदी पर हैं,
खासुलखास मंच पर बैठे।
आयोजक-संचालक गर्वित-
ज्यों कौओं में बगुले ऐंठे।
करतल ध्वनि,
चित्रों-खबरों में
रूचि सबकी है
निज प्रचार में।
*
कुशल-निपुण अभियंता आए,
छाती ताने, शीश उठाए।
गुणवत्ता बिन कार्य हो रहे,
इन्हें न मतलब, आँख चुराए।
नीति-दिशा क्या सरकारों की?
क्या हो?, बात न
है विचार में।
*
मस्ती-मौज इष्ट है यारों,
चुनौतियों से भागो प्यारों।
पाया-भोगो, हँसो-हँसाओ-
वंचित को बिसराओ, हारो।
जो होता है, वह होने दो।
तनिक न रूचि
रखना सुधार में।
***
नवगीत:
उपयंत्री की यंत्रणा
संजीव
.
'अगले जनम
उपयंत्री न कीजो'
करे प्रार्थना उपअभियंता
पिघले-प्रगटे भाग्यनियंता
'वत्स! बताओ, मुश्किल क्या है?
क्यों है इस माथे पर चिंता?'
'देव! प्रमोशन एक दिला दो
फिर चाहे जो काम करा लो'
'वत्स न यह संभव हो सकता
कलियुग में सच कभी न फलता'
तेरा हर अफसर स्नातक
तुझ पर डिप्लोमा का पातक
वह डिग्री के साथ रहेगा
तुझ पर हरदम वार करेगा
तुझे भेज साईट पर सोये
तू उन्नति के अवसर खोये
तू है नींव कलश है अफसर
इसीलिये वह पाता अवसर
जे ई से ई इन सी होता
तू अपनी किस्मत को रोता
तू नियुक्त होता उपयंत्री
और रिटायर हो उपयंत्री
तेरी मेहनत उसका परचम
उसको खुशियाँ, तुझको मातम
सर्वे कर प्राक्कलन बनाता
वह स्वीकृत कर नाम कमाता
तू साईट पर बहा पसीना
वह कहलाता रहा नगीना
काम करा तू देयक लाता
वह पारित कर दाम कमाता
ठेकेदार सगे हैं उसके
पत्रकार फल पाते मिलके
मंत्री-सचिव उसी के संग हैं
पग-पग पर तू होता तंग है
पार न तू इनसे पायेगा
रोग पाल, घुट मर जाएगा
अफसर से मत, कभी होड़ ले
भूल पदोन्नति, हाथ जोड़ ले
तेरा होना नहीं प्रमोशन
तेरा होगा नहीं डिमोशन
तू मृत्युंजय, नहीं झोल दे
उठकर इनकी पोल खोल दे
खुश रह जैसा और जहाँ है
तुझसे बेहतर कौन-कहाँ है?
पाप कट रहे तेरे सारे
अफसर को ठेंगा दिखला रे!
बच्चे पढ़ें-बढ़ेंगे तेरे
तब संवरेंगे सांझ-सवेरे
अफसर सचिवालय जाएगा
बाबू बनकर पछतायेगा
कर्म योग तेरी किस्मत में
भोग-रोग उनकी किस्मत में
कह न किसी से कभी पसीजो
श्रम-सीकर में खुश रह भीजो
…
सलिल.संजीव@जीमेल.कॉम
http://divyanarmada.blogspot.com
http://hindihindi.in




