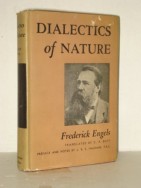सामायिक शोधलेख :
इतिहास के मिथक तोड़ती तकनीक
प्रमोद भार्गव

विज्ञान
सम्मत कोई भी नई मान्यता वर्तमान मान्यता के खण्डन के दृष्टिगत
अस्तित्व में लाई जाती है। नई मान्यता का उत्सर्जन पहली मान्यता से
दूसरी मान्यता के बीच सामने आए नए तथ्यों, साक्ष्यों, जैविक कारणों और
नई तकनीकी विधियों से संभव होता है। इस दृष्टि से भारत की भारतीयता,
अखण्डता व संप्रभुता को मजबूती प्रदान करने वाले तकनीकी माध्यम से किए गए
तीन शोधपरक अध्ययन सामने आए हैं। पहला जो एकदम नया अध्ययन है का
निर्ष्कष है कि आर्यों के बहार से भारत आने की कहानियां गढ़ी हुई हैं। यह
शोध हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एण्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने किया
है। इस शोध का आधार अनुवांशिकी (जेनेटिक्स) है। एक दूसरे अध्ययन में दो
साल पहले डीएनए की विस्तृत जांच से खुलासा किया गया था कि देश के
बहुसंख्यक लोगों के पूर्वज दक्षिण भारतीय दो आदिवासी समुदाय हैं। मानव
इतिहास विकास के क्रम में यह स्थिति जैविक क्रिया के रुप में सामने आई
हैं। वैसे भी इतिहास अब केवल घटनाओं और तिथियों की सूचना भर नहीं रह गया
है। तीसरे अध्ययन ने निश्चित किया है कि भगवान श्रीकृष्ण हिन्दू मिथक
और पौराणिक कथाओं के काल्पनिक पात्र न होकर एक वास्तविक पात्र थे और
कुरुक्षेत्र के मैदान में वास्तव में महाभारत युद्ध लड़ा गया था। भारतीय
परिदृश्य या परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त मान्यताएं स्वीकार ली जाती हैं
तो शायद मिथक बना दिए गए राम और कृष्ण जैसे संघर्षशील नायकत्व-चरित्रों
से ईश्वरीय अवधारणा की मिथकीय केंचुल उतरे। हमारे संज्ञान में अब यह
वैज्ञानिक सच आ ही गया है कि हम भारतीय उपमहाद्वीप के ही आदिवासी समूहों के
वंशज हैं, फिर यह धर्म, जाति, संप्रदाय व भाषाई विभाजक लकीर क्यों ?
लेकिन क्या ये जड़ों की ओर लौटने का संकेत देने वाले अनुसंधानपरक
वैज्ञानिक चिंतन ईश्वरीय, सृष्टि की काल्पनिक अवधारणा को चुनौती देते
हुए भारतीय समाज को बदल पाएंगे ?
प्रसिद्ध जीव विज्ञानी चार्ल्स
डारविन ने उन्नीसवीं सदी के मध्य में विकासवाद के सिद्धांत को स्थापित
करते हुए बताया था कि पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और यहां तक की मनुष्य भी हमेशा
से आज जैसे नहीं रहे हैं, बल्कि वे बेतरतीब बदलाव (रैन्डम म्यूटेशन) और
प्राकृतिक चयन (नेचुरल सिलेक्शन) द्वारा निम्नतर से उच्चतर जीवन की ओर
विकसित होते रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया की जिस खास प्रजाति
से मानव का विकास हुआ, उसके संबंधी आज भी अफ्रीका में जीवित हैं। इसलिए इस
सिद्धांत को मानने में किसी सवर्ण में यह हीनता-बोध पैदा नहीं होना चाहिए
कि हमारे पुरखे आदिवासी थे।
चार्ल्स डारविन ने एच.एम.एस बीगल जहाज
पर सवारी करते हुए दुनियाभर की सैर की और कई जीव-जंतुओं का इस दृष्टि से
अध्ययन किया, जिससे सजीवों में परिवर्तन की खोज की जा सके। लिहाजा बीगल
यात्रा के दौरान वे इक्वेडॉर तट के नजदीक गैलापैगोस द्वीप समूह के कई
द्वीपों पर गए। यहां उन्हें फिंच नाम की चिड़िया के प्रसंग में विशेष बात
यह नजर आई कि यह चिड़िया पाई तो हरेक द्वीप में जाती है, लेकिन इनमें
शारीरिक स्तर पर तमाम भिन्नताएं हैं। विशेष तौर से इनकी चोचों की आकृति
में बदलाव प्राकृतिक चयन और आहारजन्य उपलब्धता के आधार पर डारविन ने
रेखांकित किया। बाद मे यें पक्षी अलग-अलग स्थानों पर इतने भिन्न रुपों
में विकसित हो गए कि इन्हें मनुष्यों ने नई-नई प्रजातियों के रुप में ही
जाना।
समस्त भारतीय दो आदिवासी समूहों की संतानें हैं, यह भारत में
किया गया ऐसा अंनूठा अध्ययन है जिसमें शोधकर्ताओं ने भारतीय सभ्यता की
पहचान मानी जाने वाली जाति व्यवस्था पर आर्य आक्रमणकारियों के सिद्धांत
को सर्वथा नजरअंदाज किया है। अध्ययन दल के निदेशक लालजी सिंह ने इस प्रसंग
का खुलासा करते हुए स्पष्ट भी किया कि आर्य व द्रविड़ (अनार्य) के बारे
में अलग-अलग बात करने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा भी जाति सूचक रुप
में पहली बार ‘आर्य' शब्द का प्रयोग जर्मन विद्वान मेक्समुलर ने किया था।
वरना हमारी जातियों का प्रादुर्भाव तो देश के कबिलाई समूहों से हुआ है।
‘सेंटर
फॉर सेल्युलर एंड मॉलीक्युलर बायोलॉजी' (सीसीएमबी) हैदराबाद के
वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस अध्ययन में बताया गया है कि दक्षिण भारतीय
पूर्वज 65 हजार वर्ष पूर्व और उत्तर भारतीय पूर्वज 45 हजार वर्ष पूर्व
भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। देश की 1.21 अरब जनसंख्या, 4600 अलग-अलग
जातियों, धर्मों व बोलियों के आधार पर विभाजित हैं, बावजूद उनमें गहरी
अनुवांशिक समानताएं हैं। लिहाजा निम्नतम और उच्चतम जातियों के पुरखे और
उनके रक्त समूह एक ही हैं। गोया, यह खोज इस पारंपरिक अवधारणा को
अस्वीकारती है कि सभी जीव प्रजातियां अपरिवर्तन हैं और ये ईश्वरीय रचनाएं
हैं।
हालांकि इतिहास की गतिशीलता को मानव समाज की जैविक
प्रवृत्तियों से तलाशने की कोशिश मनुष्य के आदि पूर्वज ‘‘आस्टेलोपिथिक्स
रामिदस'' की खोज के रुप में ड़ेढ़ दशक पूर्व सामने आ चुकी है। धरती के इस
पहले मनुष्य की खोज इथियोपिया क्षेत्र के आरामिस के शुरुआती प्लायोसिन
चट्टानों में मिले रामिदस प्रजाति के सत्तरह सदस्यों के दांतो, खोपड़ी के
टुकड़ों और अन्य अवशेषों की उम्र 45 लाख वर्ष से अधिक आंकी गई है।
इथियोपिया के अफारी लोगों की भाषा में ‘‘रामिद'' का अर्थ होता है मूल या
जड़। रामिदस के अवशेषों के खोज कर्ता वैज्ञानिक जिसे मनुष्य और चिपांजी
जैसे नर वानरों के समान पूर्वज तथा अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन मानव पूर्वज
के जीवाश्म मानते हैं। वैज्ञानिको का दावा है कि यदि यह सही है तो इसे
इंसान की मूल प्रजाति मानना होगा।
इस शोध की बड़ी उपलब्धि
अंग्रेजों द्वारा प्रचलन में लाई गई आर्य-द्रविड़ अवधारणा भी है। जिसके तहत
बड़ी चतुराई से अंग्रेजों ने कल्पना गढ़कर तय किया कि आर्य भारत में बाहर
से आए। मसलन आर्य विदेशी थे। पाश्चात्य इतिहास लेखकों ने पौने दो सौ साल
पहले जब प्राच्य विषयों और प्राच्य विद्याओं का अध्ययन शुरु किया तो
उन्होंने कुटिलतापूर्वक ‘आर्य' शब्द को जातिसूचक शब्द के दायरे में बांध
दिया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे आर्यों को अभारतीय घोषित किया जा सके।
जबकि वैदिक युग में ‘आर्य' और ‘दस्यु' शब्द पूरे मानवीय चरित्र को दो
भागों में बांटते थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य में भारतीय नारी अपने पति
को ‘आर्य-पुत्र' अथवा ‘‘आर्य-पुरुष'' नाम से संबोधित करती थी। इससे यह
साबित होता है कि आर्य श्रेष्ठ पुरुषों का संकेतसूचक शब्द था। ऋग्वेद,
रामायण, महाभारत, पुराण व अन्य प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी आर्य शब्द का
प्रयोग जातिवाचक शब्द के रुप में नहीं हुआ है। आर्य का अर्थ ‘श्रेष्ठि'
अथवा ‘श्रेष्ठ' भी है। वैसे भी वैदिक युग में जाति नहीं वर्ण व्यवस्था
थी।
इस सिलसिले में डॉ. रामविलास शर्मा का कथन बहुत महत्वपूर्ण है,
जर्मनी मेंं जब राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ तो उनका मानना था कि हम लोग
आर्य हैं। इसलिए उन्होने जो भाषा परिवार गढ़ा था उसका नाम ‘इंडो-जर्मेनिक'
रखा। बाद में फ्रांस और ब्रिटेन वाले आए तो उन्होंने कहा कि ये जर्मन सब
लिए जा रहे हैं, सो उन्होंने उसका नाम ‘इंडो-यूरोपियन' रखा। मार्क्स 1853
में जब भारत संबंधी लेख लिख रहे थ,े उस समय उन्होंने भारत के लिए लिखा है
कि यह देश हमारी भाषाओं और धर्मों का आदि स्त्रोत है। इसलिए 1853 में यह
धारणा नहीं बनी थी कि आर्य भारत में बाहर से आए। 1850 के बाद जैसे-जैसे
ब्रिटिश साम्राज्य सुदृढ़ हुआ और फ्रांसीसी व जर्मन भी यूरोप एवं अफ्रीका
में अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तब उन्हें लगा कि ये लोग हमसे
प्राचीन सभ्यता वाले कैसे हो सकते हैं, तब उन्होंने यह सिद्धांत गढ़ा कि
एक आदि इंडो-यूरोपियन भाषा थी, उसकी कई शाखाएं थीं। एक शाखा ईरान होते हुए
यहां पर पहुंची और फिर इंडो-एरियन जो थी, वह इंडो-ईरानियन से अलग हुई और
फिर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी यह सिलसिला चला। इस कारण आर्य भारत
के मूल निवासी थे, यह गलत है। भाषाओं के इतिहास से भी इसकी पुष्टि नहीं
होती। अंततः रामविलास शर्मा ने अपने शोधों के निचोड़ में पाया कि आर्य
उत्तर भारत के ही आदिवासी थे। अर्थात ज्यादातर भारतीयों के जन्मदाता
आदिवासी समूह थे।
बंगाली इतिहासकार ए.सी.दास का मानना है कि आर्यों
का मूल निवास स्थान ‘सप्त-सिंधु' या पंजाब में था। सप्त-सिंधु में सात
नदियां बहती थीं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती।
आर्य सप्त सिंधु से ही पश्चिम की ओर गए और पूरी दुनिया में फैले।
सप्त-सिंधु के उत्तर में कश्मीर की सुंदर घाटी, पश्चिम में गांधार
प्रदेश, दक्षिण में राजपूताना, जो उस समय रेगिस्तान नहीं था और पूर्व में
गंगा का मैदान था। सप्त-सिंधु से गांधार और काबुल के मार्ग से आर्यों के
समूह पश्चिम में यूरोप और रुस गए।
पाश्चात्य और भारतीय विद्वान
भाषा वैज्ञानिक समरुपता के कारण ऐसी अटकलें लगाए हुए हैं कि आर्य विदेशों
से भारत आए। गंगाघाटी से आर्यावर्त तक की भाषाएं एक ही आर्य परिवार की आर्य
भाषाएं हैं। इसी कारण इन भाषाओं में लिपि एवं उच्चारण की भिन्नता होने
के बावजूद अपभ्रंशी समरुपता है। इससे यह लगता है कि आदिकाल में एक ही
परिवार की भाषाएं बोलने वाले पूर्वज कहीं एक ही स्थान पर रहते होंगे जो
सप्त-सिंधु ही रहा होगा। भाषा वैज्ञानिक समरुपता किसी हद तक परिकल्पना और
अनुमान की बुनियाद पर भी आधारित होती है और अब भाषा वैज्ञानिकों की यह
अवधारणा भी बन गई है कि भाषाई एकरुपता किसी जाति की एकरुपता साबित नहीं हो
सकती। इसलिए यूरोपीय जातियों के साथ भारतीय आर्यों को जोड़ना कोरी कल्पना
है। वैसे भी आर्य शब्द का प्रयोग संस्कृत साहित्य में सबसे ज्यादा हुआ
है और संस्कृत का परिमार्जित विकास भी क्रमशः भारत में ही हुआ है। इसलिए
आयोंर् का उत्थान, आर्यों का दैत्यों में विभाजन और उनकी सभ्यता,
संस्कृति और उनका पारंपरिक विस्तार के सूत्रपात के मूल में भारत ही है।
इसीलिए भारत आर्यावर्त कहलाया आर्य भारत के ही मूल निवासी थे इस तारतम्य
में 1994 में भी एक अध्ययन हुआ था। जिसके जनक भारतीय अमेरिकी विद्वान थे।
इस अध्ययन ने दावा किया था कि भारत से ही आर्य पश्चिम-एशिया होते हुए
यूरोप तक पहुंचे। इस अध्ययन का आधार पुरातात्विक अनुसंधानों, भू-जल
सर्वेक्षण, उपग्रह से मिले चित्र, प्राचीन शिल्पों की तारीखें तथा
ज्यामिति एवं वैदिक गणित रहे थे।
इस अध्ययन दल में अमेरिका की
अंतरिक्ष संस्था नासा के तात्कालिक सलाहकार डॉ. एन.एस.राजाराम, डेविड
फ्रांवले, जार्ज फयूरिस्टीन, हैरी हिक्स, जैम्स शेफर और मार्क केनोयर
शामिल थे। भारतीय अमेरिकी इतिहासविदों ने सच की तह तक पहुचने के लिए खोजबीन
की चौतरफा रणनीति अपनाई। प्रमाणों के लिए बीसवीं शताब्दी के उपलब्ध
अत्याधुनिक संसाधनों का सहारा लिया। डॉ. राजाराम ने अपना अभिमत प्रकट करते
हुए कहा है कि 19 वीं शताब्दी के भाषाशास्त्र के सिद्धांत, ऐसा ऐतिहासिक
परिदृश्य खींचते हैं, जो पिछले दो हजार साल की भारतीय परंपरा को खारिज
करने की सलाह देता है। दूसरी ओर भारतीय अमेरिकी इतिहासज्ञों का मत है कि
परंपराओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और इतिहास के मॉडलों को सुधारा जाना
चाहिए। यदि नए सबूत उनके विपरीत हों तो उन मॉडलों को नामंजूर भी किया जा
सकता है। इस आधार को सामने रखकर उन्होंने भारतीय इतिहास की जड़ों की ओर
लौटना शुरु किया तो पाया कि महाभारत का समय ईसा से 3102 साल पहले के आसपास
का था। इस काल का निर्धारण कई तरह से किया गया। महाभारत के इस काल को मिथक
नहीं माना जा सकता क्योंकि उपग्रह से मिले चित्रों से पता चलता है कि
सरस्वती नदी 1900 ईसा पूर्व सूख गई थी। महाभारत के वर्णनों में सरस्वती
का जिक्र मिलता है। लिहाजा यह भी नहीं माना जा सकता कि भारतीयों ने
ज्यामिति, यूनानियों से उधार ली थी। हड़प्पा के नगरों का नियोजन और
वास्तुशिल्प उच्चकोटि के ज्यामितिशास्त्र का प्रतिफल हैं। इस प्रमेय
को पाइथागोरस से दो हजार साल पहले बैधायन ने अपने सुलभ सूत्र में कर दिया
था।
सुलभ सूत्र में हवन-कुंड की जो ज्यामिति दी गई है, वह तीन हजार
ईसा पूर्व के हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में पाई जाती है। सूत्रों के
रचयिता अश्वालयन ने महाभारत के प्राचीन ऋषियों का उल्लेख किया है और
इन्हीं सूत्रों को हड़प्पा सभ्यता के समय साकार रुप में पाया गया।
हड़प्पा के शहर 2700 ईसा पूर्व में जिस समय अपने गौरव के चरम पर थे, उससे
कहीं पहले महाभारत का युद्ध हुआ था।
इन सब ठोस प्रमाणों के आधार पर
इन इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के सूत्र 3102 ईसा पूर्व में हुए
महाभारत से पकड़ना शुरु किए। इससे यह तर्क अपने आप खारिज हो जाता है कि
सभ्यता का अंकुरण तीन हजार ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया से हुआ। इससे करीब
एक हजार साल पहले तो ऋग्वेद पूर्ण हो गया था। ऋग्वेद काल की शुरुआत इससे
कहीं पहले हो गई थी। लोकमान्य तिलक और डेविड फ्रांवले जैसे वैदिक
विद्वानों ने ऋग्वेद में छह हजार ईसा पूर्व की तारीखों के संकेत भी खोजे
हैं।
डॉ. राजाराम ऋग्वेद काल को 4600 ईसा पूर्व मानने में कोई
कठिनाई महसूस नहीं करते। यह वह समय था जब मान्धात्र नाम के भारतीय सम्राट
ने ध्रुयू कहलाने वाले लोगों पर उत्तर-पश्चिम में कई आक्रमण किए। इन
आक्रमणों के कारण उत्तर-पश्चिम से भारी संख्या में पलायन हुआ और ये लोग
मध्य-एशिया और यूरोप तक गए। मध्य-एशिया, यूरोप और भारत के बीच भाषाई और
मिथकीय समानताओं के लिए इसे प्रमुख कारण माना जा सकता है। भारत का
उत्तर-पश्चिम का इलाका प्राचीन काल में उथल-पुथल का केन्द्र था।
मान्धात्र
के बाद राजा सूद को धु्रयू और दूसरे लोगों से जूझना पड़ा। फिर तेन राजाओं
की लड़ाइयां भी हुईं, जिनका ऋग्वेद के सांतवें खण्ड में वशिष्ठ ने भी
वर्णन किया है। प्राचीन इतिहास का यह महत्वपूर्ण दौर था। सूद राजा की
लड़ाई ने पृथुपठवा, परसू और एलिना लोगों को खदेड़ दिया। बाद में परसू लोग
फारसी कहलाए और एलिना लोग यूनानी कहलाए। सूद के दूसरे प्रतिद्वंद्वियों में
पक्था और बलहन भी शामिल थे। बाद में उनकी पीढ़ियाँ पठान या पख्तूनी और
बलूची कहलाईं। भाषाई और संस्कृति विश्लेषक श्रीकांत तलगरी ने भी इसका
वर्णन किया है। इन तथ्यों के उजागर होने से साबित हुआ कि यह सिद्धांत एकदम
खोखला है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था। ये प्रमाण और धटनाएं
सिद्धांत के एकदम विपरित यह गवाही देती हैं कि आर्य जाति का मूल स्थान
भारत था और फिर उनकी जड़ें यूरोप तक फैले वैदिक भूभाग में राजनैतिक
उथल-पुथल के कारण आर्यों का यहां से पलायन हुआ था न कि वे बाहर से आक्रांता
के रूप में यहां आए थे।
अमेरिकी मानव वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता
डॉ. जे. मार्क केनोयर भी हड़प्पा में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के बाद
लगभग यही दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। डॉ. केनोयर का मत है कि
‘भारोपीय';इंडो-यूरोपियनद्ध तथा ‘भारतीय आर्य' ;इंडा- आर्यनद्ध की
परिकल्पनाओं के पीछे यूरोपीय विद्वानों का उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता
प्रतिपादित करना था और इसके लिए उन्हें स्थितियां भी अनुकूल मिलीं।
क्योंकि तत्कालीन भारतीय मानस हीन भावना से इतना अधिक ग्रस्त था कि वह
स्वयं को पश्चिम से किसी न किसी रुप में जोड़कर ही आत्मगौरव महसूस करने
लगा था।
दरअसल पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय
अन्वेषणकर्ता डी.आर.साहनी और आर.डी. बनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा और
मोहनजोदड़ों की खोज से पहले तक पश्चिमी विद्वान यही कहते आए थे कि बाहर से
आए आर्यों ने भारत को सभ्यता से परिचित कराया। हालांकि इन खोजों से
पश्चिमी विद्वानों का यह दावा ध्वस्त हो गया, फिर भी यही मान्यता बनी
रही कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने सिंधु घाटी के मूल निवासियों को
दक्षिण एवं पूर्व की ओर खदेड़ दिया। साथ ही यह अवधारणा भी गढ़ी कि आर्य
बर्बर थे। नतीजतन हड़प्पावासी द्रविड़ उनके सामने टिक नहीं पाए। क्योंकि
आर्यों के पास अश्वों की गति और लोहे की शक्ति थी। जबकि हड़प्पा के लोग
इनसे अपरिचित थे।
डॉ केनोयर इस अवधारणा को निरस्त करते हुए कहते
हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े विभिन्न स्थलों पर 3100 वर्ष से भी
अधिक पुराने लोहे मिले हैं। जबकि बलूचिस्तान में सबसे पुराना लोहा लगभग
पौने तीन हजार साल से भी पहले का पाया गया है। इसी तरह सिंधु घाटी में
घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस तथ्य को झुठलाते हैं कि
हड़प्पावासी अश्वों से परिचित नहीं थे। डॉ. केनोयर ने माना है कि अनेक
धर्मों और जातियों के लोग हड़प्पा में एक साथ रहते थे। ‘आर्य' शब्द की
अर्थ-व्यंजना ‘सुसभ्य' और ‘सुसंस्कृत' से जुड़ी थी। फलस्वरुप जिनका
उच्च रहन-सहन व शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप था वे ‘आर्य' और जो
दबे-कुचले व सत्ता से दूर थे, ‘‘अनार्य‘‘ हुए।
अब जो आर्यों के ऊपर
अनुवांशिकी के आधार पर नया शोध सामने आया है, उससे तय हुआ है कि भारतीयों
की कोशिकाओं का जो अनुवांशिकी ढांचा है, वह बहुत पुराना है। पांच हजार साल
से भी ज्यादा पुराना है। तब यह कहानी अपने आप बे-बुनियाद साबित हो जाती है
कि भारत के लोग 3.5 हजार साल पहले किसी दूसरे देश से यहां आए थे। यदि आए
होते तो हमारा अनुवांशिकी ढांचा भी 3.5 हजार साल से ज्यादा पुराना नहीं
होता, क्योंकि जब वातावरण बदलता है तो अनुवांशिकी ढांचा भी बदल जाता है।
इस तथ्य को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हमारे बीच कोई व्यक्ति
आज अमेरिका या ब्रिटेन जाकर रहने लग जाए तो उसकी जो चौथी-पांचवीं पीढ़ी
होगी, उसका सवा-डेढ़ सौ साल बाद अनुवांशिकी सरंचना अमेरिकी या ब्रिटेन
निवासी जैसी होने लग जाऐगी। क्योंकि इन देशों के वातावरण का असर उसकी
अनुवांशिकी सरंचना पर पड़ेगा। इस शोध के बाद देखना यह है कि दुनियाभर के
जिज्ञासुओं को आर्यों के मूल निवास स्थान का जो सवाल मथ रहा है उसका कोई
परिणाम निकलता है अथवा नहीं ?
सिंधु घाटी की सभ्यता प्राचीन नगर
सभ्यताओं में एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो भगवान महावीर और महात्मा गांधी
के अंहिसावादी दर्शन की विलक्षणता व महत्ता को रेखांकित करती है। मिश्र से
लेकर सुमेरू तक की प्राचीन सभ्यताओं से ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं, जिनमें
राजा अथवा उसके दूत लोगों को मारते-पीटते दिखाए गए हैं। जबकि इसके विपरीत
सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा एक भी अवशेष नहीं मिला, इससे जाहिर होता है
कि दुनिया की यह एकमात्र ऐसी अद्वितीय सभ्यता थी, जहां आमजन पर अनुशासन
तथा अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सैन्य-शक्ति का सहारा नहीं
लिया जाता था। शासन-व्यवस्था की इस अनूठी पद्वति के विस्तृत अध्ययन की
दरकार है।
डॉ. केनोयर का मानना था कि प्राचीन भारतीय सभ्यता केवल
सिंधु घाटी में ही नहीं पनपी, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समांनातर एक
अन्य सभ्यता घाघरा-हाकड़ा में भी पनपी। ज्ञातव्य है कि सरस्वती इसी
घाघरा की शाखा थी। उन्होंने दावा किया था कि हरियाणा स्थित राखीगढ़ी तथा
पाकिस्तान के गनवेरीवाला आदि क्षेत्रों में हुए अन्वेषण कार्यों में इस
तथ्य की पुष्टि हुई है।
प्रागैतिहासिक भारत में राजनीति और धर्म,
भिन्न नहीं थे। हड़प्पा-मोहन जोदड़ो आदि राज्यों के शासक अपने रक्त
संबंधियों अथवा रिश्तेदारों के साथ राज-काज चलाते थे। यह व्यवस्था धर्म
से संचालित व नियंत्रित थी। शासक कुटुम्ब में जब सदस्यों की जनसंख्या
बढ़ जाती थी तो उनमें से एक समूह आमजनों की टोली के साथ कहीं और जा बसता
था। इन कारणों से भी एक ही भाषा-समूहों का विस्तार हुआ। इतिहास हमारे
मस्तिष्क की आंख खोल देने वाला सत्य होता है। इसलिए इनकी रचना में ज्ञान
की समस्त देन का उपयोग होना चाहिए। इस नाते भारतवंशी ब्रितानी शोधकर्ता
डॉ. नरहरि अचर ने खगोलीय घटनाओं और पुरातात्विक व भाषाई साक्ष्यों के
आधार पर दावा किया है कि भगवान कृष्ण हिन्दू मिथक व पौराणिक कथाओं के
दिव्य व काल्पनिक पात्र न होकर एक वास्तविक पात्र थे। डॉ. अचर ब्रिटेन
में टेनेसी के मेम्फिस विश्वविद्यालय में भौतिकशास्त्र के प्राध्यापक
हैं। डॉ. अचर की इस उद्घोषणा से जुड़े शोध-पत्र में खगोल विज्ञान की मदद
से महाभारत युद्ध की घटनाओं की कालगणना की है। इस शोध-पत्र का अध्ययन जब
ब्रिटेन में न्यूक्लियर मेडीसिन के फिजीशियन डॉ. मनीष पंडित ने किया तो
उनकी जिज्ञासा हुई कि क्यों न तारामंडल संबंधी सॉफ्टवेयर की मदद से डॉ.
अचर के निष्कर्षों की पड़ताल व सत्यापन किया जाए। घटनाओं की कालगणना करने
के दौरान वे उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने डॉ. अचर के शोध-पत्र
और तारामंडलीय सॉफ्टवेयर से सामने आए निष्कर्ष में अद्भुत समानता पाई।
इस
अध्ययन के अनुसार कृष्ण का जन्म ईसा पूर्व 3112 में हुआ। विश्व
प्रसिद्ध कौरव व पाण्डवों के बीच लड़ा गया महाभारत युद्ध ईसा पूर्व 3067
में हुआ। इन काल-गणनाओं के आधार पर महाभारत युद्ध के समय कृष्ण की उम्र
54-55 साल की थी। महाभारत में 140 से अधिक खगोलीय घटनाओं का विवरण है। इसी
आधार पर डॉ. नरहरि अचर ने पता लगाया कि महाभारत युद्ध के समय आकाश कैसा था
और उस दौरान कौन-कौन सी खगोलीय घटनाएं घटी थीं। जब इन दोनों अध्ययनों के
तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले गए तो पता चला कि महाभारत युद्ध ईसा पूर्व 22
नवंबर 3167 को शुरु होकर 17 दिन चला था। इन अध्ययनों से निर्धारित होता है
कि कृष्ण कोई अलौकिक या दैवीय शक्ति न होकर एक मानवीय पौरुषीय शक्ति
थे। डॉ. मनीष पंडित इस अध्ययन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ‘कृष्ण
इतिहास और मिथक' नाम से एक दस्तावेजी फिल्म भी बना डाली।
इन
तथ्यपरक अध्ययनों के सामने आने के बाद अब जरुरी हो जाता है कि हम अपनी उस
मानसिकता को बदलें, जिसके चलते हमने प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और
साहित्य के प्रति तो सख्त रवैया अपनाया हुआ है और औपनिवेशिक पाश्चात्य
संप्रभुता के प्रति दास वृत्ति के अंदाज में कमोवेश लचीला रुख अपनाया हुआ
है। अंग्रेज व उनके निष्ठावान अनुयायी भारतीय बौद्धिकों ने आर्य-अनार्य,
आर्य-दस्यु और आर्य द्रविड़ समस्याएं खड़ी करके यह सिद्ध करने की कोशिश
की है कि भारत आदिकाल से ही विदेशी जातियों का उपनिवेश रहा है। इस बात से
वे यह भी सिद्ध करना चाहते थे कि भारत पर ब्रितानी साम्राज्य का आधिपत्य
सर्वथा वैद्य होते हुए न्यायसंगत था। लेकिन अब समय आ गया है कि इस मानसिक
जड़ता को बदला जाए। यदि धर्म, भाषा, जाति और सांप्रदायिक सोच से ऊपर उठकर
हम अपनी दृष्टि में साक्ष्य आधारित परिवर्तन कालांतर में लाते हैं तो देश
असभ्यता व अज्ञानता के हीनता-बोध से तो उबरेगा ही हमारे ऐतिहासिक,
सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों में भी क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
प्रमोद भार्गव
शब्दार्थ 49,श्रीराम कॉलोनी
शिवपुरी (म.प्र.) पिन 473-551
मो. 09425488224 फोन 07492-232007, 233882
ई-पता pramodsvp997@rediffmail.com
pramod.bhargava15@gmail.com