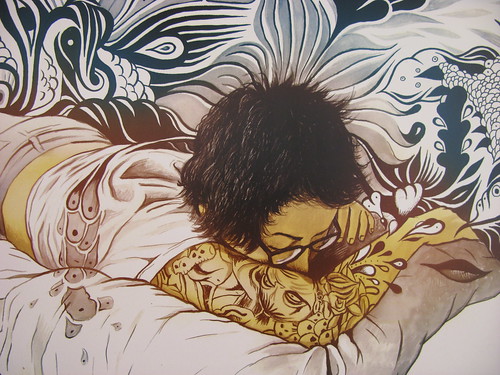काव्य का रचना शास्त्र : १
ध्वनि कविता की जान है...
- आचार्य संजीव 'सलिल'

ध्वनि कविता की जान है, भाव श्वास-प्रश्वास.
अक्षर तन, अभिव्यक्ति मन, छंद वेश-विन्यास..
अपने उद्भव के साथ ही मनुष्य को प्रकृति और पशुओं से निरंतर संघर्ष करना पड़ा. सुन्दर, मोहक, रमणीय प्राकृतिक दृश्य उसे रोमांचित, मुग्ध और उल्लसित करते थे. प्रकृति की रहस्यमय-भयानक घटनाएँ उसे डराती थीं. बलवान हिंस्र पशुओं से भयभीत होकर वह व्याकुल हो उठता था. विडम्बना यह कि उसका शारीरिक बल और शक्तियाँ बहुत कम थीं. अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसके पास देखे-सुने को समझने और समझाने की बेहतर बुद्धि थी. बाह्य तथा आतंरिक संघर्षों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने और अन्यों की अभिव्यक्ति को ग्रहण करने की शक्ति का उत्तरोत्तर विकास कर मनुष्य सर्वजयी बन सका.
 रचनाकार परिचय:-
रचनाकार परिचय:-आचार्य संजीव वर्मा 'सलिल' नें नागरिक अभियंत्रण में त्रिवर्षीय डिप्लोमा. बी.ई.., एम. आई.ई., अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र में एम. ऐ.., एल-एल. बी., विशारद,, पत्रकारिता में डिप्लोमा, कंप्युटर ऍप्लिकेशन में डिप्लोमा किया है। आपकी प्रथम प्रकाशित कृति 'कलम के देव' भक्ति गीत संग्रह है। 'लोकतंत्र का मकबरा' तथा 'मीत मेरे' आपकी छंद मुक्त कविताओं के संग्रह हैं। आपकी चौथी प्रकाशित कृति है 'भूकंप के साथ जीना सीखें'। आपनें निर्माण के नूपुर, नींव के पत्थर, राम नम सुखदाई, तिनका-तिनका नीड़, सौरभ:, यदा-कदा, द्वार खड़े इतिहास के, काव्य मन्दाकिनी २००८ आदि पुस्तकों के साथ साथ अनेक पत्रिकाओं व स्मारिकाओं का भी संपादन किया है। आपको देश-विदेश में १२ राज्यों की ५० सस्थाओं ने ७० सम्मानों से सम्मानित किया जिनमें प्रमुख हैं : आचार्य, २०वीन शताब्दी रत्न, सरस्वती रत्न, संपादक रत्न, विज्ञानं रत्न, शारदा सुत, श्रेष्ठ गीतकार, भाषा भूषण, चित्रांश गौरव, साहित्य गौरव, साहित्य वारिधि, साहित्य शिरोमणि, काव्य श्री, मानसरोवर साहित्य सम्मान, पाथेय सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान, आदि। वर्तमान में आप म.प्र. सड़क विकास निगम में उप महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं।
अनुभूतियों को अभिव्यक्त और संप्रेषित करने के लिए मनुष्य ने सहारा लिया ध्वनि का. वह आँधियों, तूफानों, मूसलाधार बरसात, भूकंप, समुद्र की लहरों, शेर की दहाड़, हाथी की चिंघाड़ आदि से सहमकर छिपता फिरता. प्रकृति का रौद्र रूप उसे डराता. मंद समीरण, शीतल फुहार, कोयल की कूक, गगन और सागर का विस्तार उसमें दिगंत तक जाने की अभिलाषा पैदा करते. उल्लसित-उत्साहित मनुष्य कलकल निनाद की तरह किलकते हुए अन्य मनुष्यों को उत्साहित करता. अनुभूति को अभिव्यक्त कर अपने मन के भावों को विचार का रूप देने में ध्वनि की तीक्ष्णता, मधुरता, लय, गति की तीव्रता-मंदता, आवृत्ति, लालित्य-रुक्षता आदि उसकी सहायक हुईं. अपनी अभिव्यक्ति को शुद्ध, समर्थ तथा सबको समझ आने योग्य बनाना उसकी प्राथमिक आवश्यकता थी.
सकल सृष्टि का हित करे, कालजयी आदित्य.
जो सबके हित हेतु हो, अमर वही साहित्य.
भावनाओं के आवेग को अभिव्यक्त करने का यह प्रयास ही कला के रूप में विकसित होता हुआ 'साहित्य' के रूप में प्रस्फुटित हुआ. सबके हित की यह मूल भावना 'हितेन सहितं' ही साहित्य और असाहित्य के बीच की सीमा रेखा है जिसके निकष पर किसी रचना को परखा जाना चाहिए. सनातन भारतीय चिंतन में 'सत्य-शिव-सुन्दर' की कसौटी पर खरी कला को ही मान्यता देने के पीछे भी यही भावना है. 'शिव' अर्थात 'सर्व कल्याणकारी, 'कला कला के लिए' का पाश्चात्य सिद्धांत पूर्व को स्वीकार नहीं हुआ. साहित्य नर्मदा का कालजयी प्रवाह 'नर्मं ददाति इति नर्मदा' अर्थात 'जो सबको आनंद दे, वही नर्मदा' को ही आदर्श मानकर सतत सृजन पथ पर बढ़ता रहा.
मानवीय अभिव्यक्ति के शास्त्र 'साहित्य' को पश्चिम में 'पुस्तकों का समुच्चय', 'संचित ज्ञान का भंडार', 'जीवन की व्याख्या', आदि कहा गया है. भारत में स्थूल इन्द्रियजन्य अनुभव के स्थान पर अन्तरंग आत्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया. यह अंतर साहित्य को मस्तिष्क और ह्रदय से उद्भूत मानने का है. आप स्वयं भी अनुभव करेंगे के बौद्धिक-तार्किक कथ्य की तुलना में सरस-मर्मस्पर्शी बात अधिक प्रभाव छोड़ती है. विशेषकर काव्य (गीति या पद्य) में तो भावनाओं का ही साम्राज्य होता है.
होता नहीं दिमाग से, जो संचालित मीत.
दिल की सुन दिल से जुड़े, पा दिलवर की प्रीत..
दिल की सुन दिल से जुड़े, पा दिलवर की प्रीत..
साध्य आत्म-आनंद है :
काव्य का उद्देश्य सर्व कल्याण के साथ ही निजानंद भी मान्य है. भावानुभूति या रसानुभूति काव्य की आत्मा है किन्तु मनोरंजन मात्र ही साहित्य या काव्य का लक्ष्य या ध्येय नहीं है. आजकल दूरदर्शन पर आ रहे कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन पर केन्द्रित होने के कारण समाज को कुछ दे नहीं पा रहे जबकि साहित्य का सृजन ही समाज को कुछ देने के लिये किया जाता है.
जन-जन का आनंद जब, बने आत्म-आनंद.
कल-कल सलिल-निनाद सम, तभी गूँजते छंद..
कल-कल सलिल-निनाद सम, तभी गूँजते छंद..
बुद्धि भाव कल्पना कला, शब्द काव्य के तत्व.
तत्व न हों तो काव्य का, खो जाता है स्वत्व..
तत्व न हों तो काव्य का, खो जाता है स्वत्व..
बुद्धि या ज्ञान तत्व काव्य को ग्रहणीय बनाता है. सत-असत, ग्राह्य-अग्राह्य, शिव-अशिव, सुन्दर-असुंदर, उपयोगी-अनुपयोगी में भेद तथा उपयुक्त का चयन बुद्धि तत्व के बिना संभव नहीं. कृति को विकृति न होने देकर सुकृति बनाने में यही तत्व प्रभावी होता है.
भाव तत्व को राग तत्व या रस तत्व भी कहा जाता है. भाव की तीव्रता ही काव्य को हृद्स्पर्शी बनाती है. संवेदनशीलता तथा सहृदयता ही रचनाकार के ह्रदय से पाठक तक रस-गंगा बहाती है.
कल्पना लौकिक को अलौकिक और अलौकिक को लौकिक बनाती है. रचनाकार के ह्रदय-पटल पर बाह्य जगत तथा अंतर्जगत में हुए अनुभव अपनी छाप छोड़ते हैं. साहित्य सृजन के समय अवचेतन में संग्रहित पूर्वानुभूत संस्कारों का चित्रण कल्पना शक्ति से ही संभव होता है. रचनाकार अपने अनुभूत तथ्य को यथावत कथ्य नहीं बनता. वह जाने-अनजाने सच=झूट का ऐसा मिश्रण करता है जो सत्यता का आभास कराता है.
कला तत्त्व को शैली भी कह सकते हैं. किसी एक अनुभव को अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं. हर रचनाकार का किसी बात को कहने का खास तरीके को उसकी शैली कहा जाता है. कला तत्व ही 'शिवता' का वाहक होता है. कला असुंदर को भी सुन्दर बना देती है.
शब्द को कला तत्व में समाविष्ट किया जा सकता है किन्तु यह अपने आपमें एक अलग तत्व है. भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम शब्द ही होता है. रचनाकार समुचित शब्द का चयन कर पाठक को कथ्य से तादात्म्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है.
दिल-दिमाग की कशमकश, भावों का व्यापार.
बनता है साहित्य की, रचना का आधार..
बनता है साहित्य की, रचना का आधार..
बुद्धि तत्त्व की प्रधानतावाला बोधात्मक साहित्य ज्ञान-वृद्धि में सहायक होता है. हृदय तत्त्व को प्रमुखता देनेवाला रागात्मक साहित्य पशुत्व से देवत्व की ओर जाना की प्रेरणा देता है. अमर साहित्यकार डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे साहित्य को 'रचनात्मक साहित्य' कहा है.
 सादर समर्पित
सादर समर्पित यह लेख श्रंखला मुझमें भाषा और साहित्य की रूचि जगानेवाली पूजनीय माता जी व प्रख्यात- आशु कवयित्री स्व. श्रीमति शांति देवी वर्मा की पुण्य-स्मृति को समर्पित है।
-संजीव
लक्ष्य और लक्षण ग्रन्थ
रचनात्मक या रागात्मक साहित्य के दो भेद लक्ष्य ग्रन्थ और लक्षण ग्रन्थ हैं साहित्यकार का उद्देश्य अलौकिक आनंद की सृष्टि करना होता है जिसमें रसमग्न होकर पाठक रचना के कथ्य, घटनाक्रम, पात्रों और सन्देश के साथ अभिन्न हो सके.
लक्ष्य ग्रन्थ में रचनाकार नूतन भावः लोक की सृष्टि करता है जिसके गुण-दोष विवेचन के लिये व्यापक अध्ययन-मनन पश्चात् कुछ लक्षण और नियम निर्धारित किये गये हैं लक्ष्य ग्रंथों के आकलन अथवा मूल्यांकन (गुण-दोष विवेचन) संबन्धी साहित्य लक्षण ग्रन्थ होंगे. लक्ष्य ग्रन्थ साहित्य का भावः पक्ष हैं तो लक्षण ग्रन्थ विचार पक्ष. काव्य के लक्षणों, नियमों, रस, भाव, अलंकार, गुण-दोष आदि का विवेचन 'साहित्य शास्त्र' के अंतर्गत आता है 'काव्य का रचना शास्त्र' विषय भी 'साहित्य शास्त्र' का अंग है.
साहित्य के रूप --
१. लक्ष्य ग्रन्थ : (क) दृश्य काव्य, (ख) श्रव्य काव्य.
२. लक्षण ग्रन्थ : (क) समीक्षा, (ख) साहित्य शास्त्र.क्रमश: .....
(आभार : साहित्य शिल्पी, मंगलवार, १० मार्च २००९)
**************