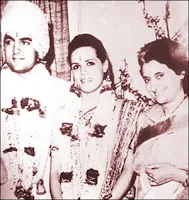जून की खिली गर्मी, जब तब काले-काले बादलों से भरा आसमान, बीच बीच में मानसूनी हवा का शरारती झोंका, जो शोध के बजाए कविता लिखने को ललचाता, लेकिन मौसम, हवा, कविता - इतनी तरह के सुहावने लोभ आसपास मंडराने पर भी, बाबू जी से मिलने का, साक्षात्कार करने का लोभ इन सब पर भारी पड़ा.
अमृतलाल नागर - जिन्हें मैं बाबू जी कह कर संबोधित करती थी, आज भी जब याद आते हैं तो एकाएक उनके ठहाके कानों में गूँज उठते हैं. जिंदादिल, उदार मनस, हँसता चेहरा, मुस्कुराती आँखें - उनकी ये खूबियाँ सिलसिलेवार आँखों में लहरा उठती हैं.

उनसे मेरी पहली मुलाक़ात मेरे शोध कार्य के दौरान सन् १९७७ में हुई थी. आगरा विश्वविद्यालय से हिन्दी एम.ए. के बाद मैंने अपने निदेशक से चर्चा के उपरांत नागर जी के उपन्यास साहित्य पर शोध करने का निर्णय लिया और अविलम्ब उनके उपन्यास खरीद कर पढने शुरू किए. उनके उपन्यास इतने हृदयग्राही थे कि शुरू करने के बाद बीच में छोडने का मन ही नहीं होता था. मेरी फुफेरी बहन जो उस समय आई.टी. कालिज, लखनऊ में फिजिक्स विभाग में प्रवक्ता थी और बहन कम सहेली अधिक थी - उसे मैंने फोन पर ‘आपातकालीन आदेश’ दिया कि किसी भी तरह जल्द से जल्द नागर जी का फोन नंबर डायरेक्टरी से या चौक में उनके घर जाकर पता करे और शीघ्र ही मुझे भेजे. मेरी दीदी ने भी मुस्तैदी से काम किया और दो दिन के अंदर बाबू जी का फोन नंबर मुझे मिल गया. फिर क्या था, मैं जो भी उपन्यास पढ़ कर खत्म करती, फोन से उस पर बाबूजी से ज़रूरी प्रश्न करती और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करती. बाबू जी भी बोलने वाले और मैं भी. जब भी फोन करती, उनके उपन्यासों के सन्दर्भ में रुचिकर बातें होतीं. लेखन के दौरान बाबू जी जिन अनमोल अनुभवों से गुज़रे थे, उन्हें बताते समय वे अतीत में डूब जाते और उनके साथ - साथ मैं भी लखनऊ, बनारस की गलियों, मौहल्लों, वहाँ के नुक्कडों और हवेलियों में पहुँच जाती. इस पर भी तृप्ति नहीं होती. लंबी बातचीत होने के बावजूद भी, उनके उपन्यासों के पात्रों और कथ्य से जुडे अनेक वर्क अनछुए रह जाते. उनके बारे में, फ़ोन करने के बजाय, मैं बाबू जी को खत लिखती. उनका बडप्पन देखिए कि बाबू जी मेरे खत की हर बात का जवाब बड़े धैर्य से देते. उनकी इस बात से मैं बहुत अधिक प्रभावित थी. इतने व्यस्त लेखक; लेकिन पत्र का उत्तर देने में तनिक भी देरी नहीं. पत्र भी कोई रोज़मर्रा की साधारण बातों वाला नहीं अपितु शोध से जुड़े विकट प्रश्नों से बिंधा पत्र और समुद्र से शांत बाबू जी बिना झुंझलाए सहजता से उत्तर लिख भेजते. उनका लेख बेहद ख़ूबसूरत और कलात्मक था. मेरे शोध कार्य में किसी तरह की वैचारिक बाधा न आए और न देरी हो - इस बात का वे हमेशा ख्याल रखते. पिता की भाँति उनका यह सोच मेरे अंतर्मन पर मीठी-मीठी अमिट छाप छोडता. एक शोधार्थी के लिए उनकी यह प्रतिबध्दता, उदारता और ख्याल, उनके सँस्कारों और उस बीते ज़माने के ऊँचे अखलाख का परिचायक था. फिलहाल उनके एक पत्र को पाठकों के साथ बाँटना चाहूँगी. बाबू जी से बातचीत होने पर, हर बार उनके व्यक्तित्व की एक नई परत खुलती और मैं उस महान हस्ती के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो उठती. मैंने लोगों से उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में सुन रखा था. लेकिन अब तक मैं स्वयं उनसे बातचीत करके जान गई थी कि वे कितनी अद्भुत हस्ती थे. उनसे बिना मिले ही, सिर्फ फोन पर बातचीत करने भर से ही उनकी सरलता और अभिजात्यता की मिश्रित तरंगें मुझ तक पहुँच चुकी थी. उनका साहित्य पढकर समाप्त करने के बाद उनसे साक्षात्कार का कार्यक्रम बना. जब मैंने बाबू जी को लिखा कि उनकी सुविधानुसार उनसे मिलने लखनऊ आना चाहूँगी तो उन्होंने मेरे आगमन का स्वागत करते हुए, सुघड़ लेख में सफ़ेद पोस्टकार्ड पर अपने घर तक सरलता से पहुँचने का मार्गदर्शन करते हुए मुझे पत्र लिख भेजा. उनसे मिलने के समय आदि का निर्णय - जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में, कभी भी; बाबू जी ने मुझ पर छोड़ दिया. उनकी इस छूट के कारण, सर्दियों से टलता हुआ प्रोग्राम गर्मी के मौसम तक पहुँच गया.

निश्चित तिथि और समय पर मैं जून में लखनऊ पहुँची और अपने फूफा श्वसुर डा. बलजीत सिंह और बुआ सरला गर्ग के घर ठहरी. वे दोनों लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफैसर थे. बुआ और फूफा जी का सुझाव था कि कि मुझे कैम्पस में उनके पास ही रहना चाहिए और साथ ही प्यार भरी धमकी भी उन्होंने दे डाली थी कि कहीं और ठहरी तो वे नाराज़ हो जाएँगे. दूसरी ओर मेरी अपनी बुआ और बहनों ने इसरार किया कि मैं उनके पास ‘चौक’ में ही ठहरूँ. वहाँ से नागर जी का घर भी पास पडेगा. दोनों ही रिश्ते निकट के थे. मुझे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में शोध से सम्बंधित रिफरेंस पुस्तके भी खोजनी थी और अध्ययन भी करना था, यह कार्य कैम्पस स्थित उनके बंगले में ठहरने पर अधिक सुविधा से हो सकता था. सो अंत में, मेरी बहनें और बुआ, मेरे शोध की ज़रूरतों को समझते हुए मेरे यूनिवर्सिटी कैम्पस में ही ठहरने की बात पर राजी हो गई. घर पहुँच कर, थोड़ा फ्रेश होकर, सबसे पहले मैंने बाबू जी को फोन किया और अपने पहुँचने की सूचना दी. जब मैंने उनसे मिलने का समय तय करने की बात करी तो वे फिर वही पितृतुल्य ममत्व से भरे हुए, आदेश देते बोले –
‘सबसे पहले, लखनऊ में तुम्हारा बहुत-बहुत स्वागत ! देखो बेटा, आज तुम पूरी तरह आराम करोगी, समझीं, सफर की थकान उतारो. कल शाम यहाँ आना, इत्मीनान से चर्चा करेगें.’
उनके स्नेह से आह्लादित सी, निरुत्तर हुई मैं उनका कहा मानने को विवश थी.
अगले दिन, मैं ठीक चार बजे चौक स्थित नागर जी के घर पहुँच गई. चौक में खुनखुन जी की कोठी से आगे एल.आई. सी. की इमारत थी, जिसके सामने वाली सड़क के दूसरी ओर मिर्ज़ा मंडी गली थी. गली में बीस कदम चलने के बाद नागर जी का मकान आ गया. घर क्या था - एक विशालकाय हवेली थी, जिसके लहीम-शहीम, पुरानी शैली वाले नक्काशीदार दरवाजे ने उदारता से मेरा स्वागत किया. उस बुलंद दरवाजे से अंदर प्रवेश कर मैंने अपने को दहलीज में खडा पाया. उस दहलीज में एक दूसरा मध्यम आकार का दरवाजा था. उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वह हँस रहा हो. उस हँसमुख दरवाजे ने आँगन में जाने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया. मैं उस दरवाज़े को ऊपर से नीचे तक देखती हुई सोचने लगी कि इसमें ऐसा क्या है जो यह मुझे इतना हँसोड़ नज़र आ रहा है...!! या बाबू जी की उन्मुक्त हँसी इसकी रग-रग में समा गई है. मन में बढ़ते प्रफुल्लता के आयतन को सम्हालती जब मैंने अंदर नज़र डाली तो - सामने फैला हुआ विशाल आँगन और उसके आगे बरामदे से लगे खुले कमरे में चौकी पर किताबों, पत्रिकाओं के जमावड़े के साथ बैठे बाबू जी आँखों पर चश्मा चढाए, एक फ़ाइल में कुछ लिखने में मशगूल नज़र आए. मैंने उनकी तन्मयता में व्यवधान डाले बिना, पहले खामोशी से उनके अदभुत घर का जायाज़ा लिया. सहन के एक किनारे पर प्रवेश द्वार, द्वार के दाईं ओर दूर रसोई, शेष दोनों ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रम से बने दुमंजले कमरों की कतार. घर के खुलेपन को और अधिक विस्तार देता, ऊपर खुला आसमान......मुझे सारा घर बाबू जी के विशाल हृदय की प्रतिछवि लगा. कमरों के चौपट खुले दरवाजे भी भरपूर मुँह खोल कर खिलखिलाते लग रहे थे. उनके साथ अधखुली खिडकियाँ मंद मंद मुस्कुराती सी लगी

हर घर की विशिष्ट तरंगें होती हैं जो घरवालों से पहले, आने वाले का स्वागत करती हैं और चुपचाप घर की आबो-हवा का, मिजाज़ का परिचय दे डालती हैं. स्वचालित इस परिचय प्रक्रिया के तहत बाबू जी के घर की खुशनुमा तरंगें मुझ तक पहुँच चुकी थीं. मै भी उनसे तरंगायित हो, बाबू जी से मिलने के उत्साह से छलकती, बिना आहट किए सधे कदम चलती, अपनी तीन साल की बेटी ‘मानसी’ की अंगुली थामे, बाबू जी के निकट पहुँच कर, उनका ध्यान भंग करती बोली – बाबू जी प्रणाम ! सुनते ही जैसे बाबू जी की तंद्रा टूटी और वे झटपट आँखों से चश्मा उतारते बोले – ‘अरे ! आ गई बेटा, दीप्ति हो न ? कहीं कोई और हो और मैं उसे दीप्ति समझ बैठूँ.’

‘नहीं कोई और नहीं, बाबू जी, आपने ठीक पहचाना ’ - यह कहती मैं उस महान हस्ती के सान्निध्य से गदगद हुई, तुरंत उनके चरणस्पर्श के लिए झुक गई. लेकिन बाबू जी ने चरणों तक पहुँचने से पहले ही, मुझे हाथों से रोक कर, आशीष दिया और बड़े सत्कार से बैठने के लिए कहा. मेरी देखा देखी, मानसी भी उकडूँ बैठ कर नन्हे-नन्हें हाथों से बाबू जी के पैर छू कर माथे से लगा कर, मेरी तरफ पलटी तो बाबू जी ने मानसी की औपचारिक शिष्टाचार की उस नकल अंदाज़ी के भोलेपन पर मुग्ध होकर उसे गोद में उठा लिया और बोले – अरे वाह ! इस नन्ही गुडिया की तहज़ीब ने तो मेरा दिल मोह लिया. फिर उसके नन्हें हाथों को चूमा और प्यार से सिर पर हाथ फेर कर मेरे पास कुर्सी पर बैठा दिया. इतने में सारा शिष्टाचार भुला कर, मानसी ने रूठते हुए तुतला कर कहा – ‘बाबा जी ने मेरे बाल खराब कर दिए....’ बस फिर क्या था – यह सुनते ही बाबू जी ने जो ठहाका लगाया तो मैं भी अपनी हँसी न रोक सकी और हमें हँसते देख, मानसी भी हँसने लगी – शायद यह सोच कर कि जब हम हँस रहे हैं तो उसे भी हँसना चाहिए. उसका पहले रूठना फिर हमारे साथ खिलखिलाना देखकर मैं और बाबू जी और अधिक हँस पड़े.
फिर, बाबू जी प्यार जताते बोले -‘यहाँ पहुँचने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई ?’

मैंने कहा – ‘बाबू जी, बिलकुल नहीं - और घर में कदम रखने पर तो आपके बाहर वाले बुलंद दरवाजे से लेकर, दहलीज और आँगन, उनमें विराजमान सारे खिड़की- दरवाजों ने जो मेरा हँसते - मुस्कुराते स्वागत किया, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती’. यह सुन कर बाबू जी खुश होते हुए, हा.. हा.....हा करके हंसने लगे. उनके खुले व्यक्तित्व के आगे मेरी बिटिया को खुलते देर नहीं लगी. मैं मन ही मन घबराई कि अब अगर इसने बोलना शुरू किया और अपनी फरमाइशें, नाज़ - नखरे फैलाने शुरू किए तो बाबू जी से मेरी चर्चा होने से रही. उधर बाबू जी अपने मसखरे हाव-भाव और मीठी बातों से उसके संकोच को भगाने पर उतारू थे. बच्चे उन्हें खासतौर से प्रिय थे. इतने में बाबू जी की पोती ‘दीक्षा’ जो मानसी से थोड़ी बड़ी रही होगी, वह बड़े और लंबे से गिलास में मेरे लिए पानी छलकाती लाई. उसे देखकर मुझे तसल्ली हुई कि चलो मानसी दीक्षा के साथ थोड़ा खेलने में लग जाएगी तो बेहतर रहेगा. बाबू जी ने दोनों की दोस्ती करा दी और दीक्षा प्यार से मानसी का हाथ थामे उसे अपने खिलौने दिखाने ले गई. उसके बाद मैंने एक पल भी बरबाद किए बिना, बाबू जी से उनके उपन्यासों, कथ्य, विविध चरित्रों औए घटनाओं पर चर्चा करनी शुरू की. बाबू जी बोले – ‘देखो बेटा, ज़रा भी हिचकना मत, जो कुछ भी तुम पूछना चाहती हो, नि:संकोच पूछना. शोध के साथ न्याय करना है तो मेरा अच्छी तरह आपरेशन करना. तुम डाक्टर बनने जा रही हो. जितना अच्छा आपरेशन करोगी, उतनी ही अच्छी डाक्टर बनोगी...’
उनके इस शब्द कौशल में ध्वनित व्यंजना ने मुझे जितना हँसाया, उतना ही प्रभावित भी किया. बाबू जी की भी बातों का जवाब नहीं था. हमारी बातें चल ही रहीं थी कि कुछ देर बाद मानसी खेल से ऊब कर दौडती हुई आई और मेरा पल्लू पकड़ कर बाबू जी से बोली – ये आपका मुँह लाल लाल कैसे हुआ ?’ बाबू जी इस बार उसके बाल बिगडने का ख्याल रखते हुए, उसके गाल छू कर बोले – ‘पान से बिटिया,’
मानसी पहले तो चुप खडी रही क्योकि वह ‘पान’ क्या होता है, जानती ही नहीं थी. फिर न जाने क्या सोच कर बोली – ‘मुझे भी अपना मुँह लाल करना है.’
फिर क्या था. मैंने बाबू जी को बहुत रोकना चाहा लेकिन बाबू जी कहाँ मानने वाले. उन्होंने तुरंत पानदान से पान का छोटा सा टुकड़ा लगा कर मानसी के मुँह में रख दिया. उसने तो इससे पहले न पान देखा था न खाया था, सो क़यामत तो आनी ही थी. पहले तो उसने खाने की कोशिश करी लेकिन जब उसे पान में कोई स्वाद नहीं आया तो तुरंत ही उसका धैर्य चुक गया और उसने टुकड़ा- टुकड़ा मुँह से निकाल कर फेंकना शुरू कर दिया. पर पान ने क्षण भर में उसके मुँह को लाल करके उसकी इच्छा ज़रूर पूरी कर दी थी. इससे पहले कि बाबू जी के अध्ययन कक्ष में जगह जगह पान के टुकड़े फेंक - फेंक कर मानसी ग़दर मचाती, मैं उसे जल्दी से नल के पास ले गई और उसके मुँह से पान के टुकड़े निकाल कर, उसका मुँह साफ़ किया. फिर भी इतनी देर में अपने मुँह के अजनबी स्वाद को वह ‘छू-छू’ करके बाहर निकालने की कोशिश में लगी रही. जब वह ऐसा करती तो कभी मैं उसे इशारे से मना करती, तो कभी तरेर कर देखती. बाबू जी उसकी नाज़ुक सी छू - छू पर खिलखिला कर हँसते तो वह सोचती कि बड़ा अच्छा काम कर रही है, फलत: वह बार-बार वैसे ही करती जाती और बाबू जी की हँसी में साथ देती. किसी तरह उसे शांत करके मैंने फिर से चर्चा शुरू की. इस बार मानसी बातें खत्म होने तक समझदार की तरह खामोश बैठी रही. अब फिर उसके सब्र का बाँध खत्म हो गया था. एकाएक मेरी गोद में चढ़ कर, उसने बाबू जी से मुखातिब होकर सवाल किया – ‘आप टाफ़ी नहीं खाते ?’

वे उसके नन्हे मुन्ने सवाल का आनंद लेते बोले – ‘नहीं बिटिया रानी हम तो नहीं खाते.’
तो मानसी पटाक से बोली – ‘मै तो खाती हूँ’ और इसके आगे किसी तरह का इंतज़ार किए बिना बेधडक बोली – मुझे टाफ़ी चाहिए...मुझे टाफ़ी खानी है...
उसकी जिद की रफ़्तार को भाँप कर मैंने उसे सम्हालते हुए कहा – ‘देखो अभी हम बाजार जाने वाले हैं. मैं तुम्हें एक नहीं, ढेर सारी टाफियाँ लेकर दूँगी, पर अभी मेरा कहना मानो. ठीक है न ?’ और मेरी यह तरकीब काम कर गई. मैंने घर लौटते समय अपना वायदा पूरा भी किया. मैंने फिर अपनी बातचीत आगे बढाई और कुछ देर बात हमारी वार्ता अंतिम छोर पर पहुँच गई. मैंने बाबू जी का आभार प्रगट किया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि बाबू जी के साथ काफी हद तक संतोषजनक चर्चा भलीभाँति पूरी हो गई थी. लेकिन साथ ही मेरा मन यह भी कह रहा था कि यह चर्चा समुद्र में बूँद की मानिंद थी क्योंकि लेखक अमृतलाल नागर और उनका बहुरंगी समृद्ध साहित्य एक ऐसे विशाल उदधि के समान था जिसमें बार बार जितने गहरे जाओ, उतनी ही तथ्यपूर्ण बातें सोचने को, मनन करने को प्रेरित करती थी. बातचीत के दौरान मैंने जब उनसे, उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों के विषय में जानना चाहा तो वे निर्लिप्त भाव से बोले -
‘बेटा, अकादमी पुरस्कार हो या, प्रेमचंद पुरस्कार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा पुरस्कार मेरे पाठकों से मिलने वाली सराहना और प्यार है. किताबों से मिलने वाली रायल्टी है. मेरी दिली तमन्ना है कि पूरी तरह सिर्फ अपने लेखन से मिलने वाली रायल्टी के बलबूते पर जीवन निर्वाह कर सकूँ.’
चलते - चलते मैं उनसे एक और अंतिम सवाल करने से अपने को न रोक सकी. मैंने पूछा कि वे तो कलम के बादशाह हैं तो उन्होंने फिल्मों का लेखन कार्य किस लिए छोड़ा ? क्योंकि वे तो बड़े सराहनीय, बड़े उम्दा संवाद और पटकथा लिख रहे थे वहाँ. मेरे इस सवाल पर, वे अतीत में डूबते हुए वे बोले – ‘ बेटा फिल्मों में लेखन का तो स्वागत है, पर ‘स्वतन्त्र लेखन’ का स्वागत नहीं है. कोई भी सच्चा लेखक और ख़ास करके मुझ जैसा मुक्त स्वभाव का लेखक अपनी कलम को किसी का गुलाम नहीं बना सकता. इसलिए ही छोड़ा आया वह माया नगरी.’
फिर भी उन्होंने अपने बंबई प्रवास के दौरान जितनी भी पटकथाएँ लिखीं, संवाद लिखे, वे उनके सिनेलेखन की प्रवीणता के परिचायक हैं. १९५३ से लेकर ५७ तक लखनऊ के आकाशवाणी केन्द्र में बतौर ड्रामा प्रोड्यूसर का पद बड़ी कुशलता से सम्हाला. किन्तु ये सब गतिविधियाँ रचनात्मक होते हुए भी, उन्हें वह सुख, वह सन्तोष नहीं दे सकीं, जो उन्हें साहित्य सृजन में मिलता था. इसलिए अंतत: इन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा कर, वे अंतिम सांस तक पूर्णतया लेखन में ही लगे रहे.

बीच में, चर्चा को ब्रेक देते हुए, बड़ी ही मोहक खिलखिलाती ‘बा’ (प्रतिभा नागर) ने बड़े प्यार से चाय नाश्ता कराया. मेरे मना करने पर भी वे एक – दो खाने की चीजों तक नहीं मानीं और चार - पाँच तरह की मिठाई - नमकीन उन्होंने मेज़ पर सजा दी. बाबू जी तो मिष्ठान्न प्रेमी, सो हमें चेतावनी देते बोले – ‘खालो भय्या, वरना मैं यह सारी मिठाई खत्म कर दूँगा.’ बा तुरंत बोली – ‘आप भूल गए क्या, मैं यही बैठी हूँ, एक मिठाई ले लीजिए बस. अपनी सेहत का ख्याल कीजिए. बाबू जी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर झुकाते बोले – ‘जो हुक्म सरकार ! देखा दीप्ति, कितनी पाबंदियों के बीच रहता हूँ. मेरी यह होम मिनिस्टर बड़ी सख्त है.’
नाश्ता करने के बाद ‘बा’ ज्यों ही रसोई से ट्रे लाने के लिए वहाँ से हटीं, बाबू जी के चहरे पर शरारत तैर गई. उन्होंने झटपट २-३ बर्फी के टुकड़े मुँह में डाल लिए. दूर से ‘बा’ की नजर बाबू जी के चुपचाप मिठाई गटकते मुँह पर टिक गई. उन्हें शायद अंदाजा रहा होगा कि उनके हटते ही बाबू जी कान्हा की तरह चोरी करेगे. उनका मिठाई से भरा मुँह देख कर बा ने भाँप लिया कि बाबू जी ने अपना मिशन पूरा कर लिया. पास आकर प्यार भरी फटकार देती बोली – ‘कर ली बेईमानी मेरे उठते ही...?’
नागर जी आँखों को गोल-गोल घुमाते बोले – ‘देखो, बात समझा करो, दीप्ति और मानसी ने तो चिड़िया की तरह खाया. मैंने देखा कि मिठाई प्लेट में उदास सी पडी, अपमानित महसूस कर रही थी. मुझे अच्छा नहीं लगा मिठाइयों की उतरी सूरत देख के, सो मैंने इन्हें कृतज्ञ करने के लिए इनका उद्धार कर दिया.’ बा हँसती हुई बोली – ‘देखा बेटा कितने उपकारी हैं...’मैं हँसती हुई उन दोनो की नोक झोंक का आनंद लेती रही.
बाबू जी जैसा ज्ञान पिपासु, जिज्ञासु, जीवंत, यायावर, अनुभवों का पिटारा, बहुपठित, बहुभाषाविज्ञ, बहुआयामी व्यक्तित्व इस दुनिया की भीड़ में मिलना दुर्लभ है. वे जीर्ण-शीर्ण अर्थहीन ‘पुरातनता’ का अनुसरण न कर, स्वस्थ व रचनात्मक ‘नवीनता’ के हिमायती थे. विचारों, कार्यों और लेखन, सभी में उनके क्रांतिकारी स्वभाव की झलक मिलती है. यहाँ तक कि उनके व्यक्तित्व में भी इसकी छाप थी. ऊँचा कद, उन्नत मस्तक,खिलता हुआ टिपिकल गुजराती गौर वर्ण, मुँह में पान की गिलौरी, हाथ में कलम, जब विचारमग्न हों तो समुद्र से गहरे, जब भावनाओं में डूबे हों तो खोए खोए मौसम से, और जब चुहल पर आए तो इतना अट्टहास, इतने ठहाके कि सारी कायनात हास-परिहास में डूब जाए. क्षण-क्षण में आते जाते विविध भावों से मुखर उनका चेहरा किसी किताब से कम न था. लेकिन विनोद का भाव अन्य सब भावों को तिरोहित कर स्थायी रूप से उनके तेजस्वी मुख मंडल पर विराजमान रहता था.

बाबू जी भांग के बड़े प्रेमी थे. मुझे याद है कि एक बार मैंने उन्हें फोन किया तो ‘बा’ ने फोन उठाया और हँसी मिश्रित व्यंग्य से मुझे बताया - ‘तुम्हारे बाबू जी भांग घोट रहे हैं ‘ तब तक यह सुनकर वे खुद फोन पर आ चुके थे, पान भरे मुँह से बोले – ‘देखो दीप्ति, मैं पक्का शिव भक्त हूँ. भांग के बिना मेरी अराधना पूरी नहीं होती और यह कह कर उन्होंने फोन पर आदत के अनुसार एक ज़ोरदार ठहाका लगाया.’
मैं तीन घंटे नागर जी के सान्निध्य में रही और उन तीन घंटों में उनसे अनवरत इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई कि जितनी तीन माह साथ रहने पर भी शायद न हो पाती. मेरे विदा लेने का समय आ गया, सो उठते हुए मैंने कृतज्ञता ज़ाहिर की और कहा – ‘बाबू जी, मैंने आपका बहुत समय लिया. वैसे तो आपने मेरी लगभग सभी जिज्ञासाओं का शमन किया, फिर भी यदि कुछ और पूछने की ज़रूरत पडी तो फोन से अथवा खत लिख कर पूछ लूँगी.’
यह सुनकर बाबू जी सुझाव देते बोले – ‘अभी कब तक हो तुम लखनऊ में ?
मैं बोली - ‘ पन्द्रह - बीस दिन तो रहना होगा और शायद पूरा जून भी रुक सकती हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ‘सन्दर्भ पुस्तकें’ खोजनी हैं, विशेष प्रसंगों का अध्ययन करना है.’
बाबू जी एकदम बोले – ‘तो कभी भी दोबारा आ जाओ न बेटा. काफी दिन हैं तुम्हारे पास.’
मैं संकोच करती बोली – ‘मन तो है एक बार फिर से आने का लेकिन आपको परेशान नहीं करना चाहती. आपकी रचनात्मकता में बाधा डालना उचित नहीं. लेखक को लेखन कितना प्रिय होता है, यह मैं समझ सकती हूँ.’
बाबू जी सिर पर हाथ फेरते बोले – ‘अब इतनी भी समझदारी अच्छी नहीं, आज हूँ दुनिया में, कल का क्या पता.. ‘ उनके ये शब्द मुझे एकाएक भावुक बना गए. और अनायास मेरे मुँह से निकल गया – बस, बाबू जी, बस ऐसा मत कहिए.’
फिर वे डपटते से बोले – ‘ अरे, बेटा साहित्यिक चर्चा और वो भी जब मेरी रचानाओं पर हो तो मैं क्यों परेशान होने लगा. मैं तो बड़ी रुचि से, आनंद के साथ तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जितनी बार चाहो, देने को तैयार हूँ.’
बाबू जी के बड़प्पन और उदारता से अभिभूत हुई मैंने एक सप्ताह बाद आने की इच्छा ज़ाहिर की तो बा और बाबू जी, दोनों एक साथ बोल पड़े – ‘तो अगली बार रात का खाना हमारे साथ खाना.’
मैंने कहा कि वे खाने का तकल्लुफ न करे. वैसे ही मुझसे उनके ख्याल और प्यार का भार नहीं सम्हाला जा रहा है ऊपर से इतनी खातिर......लेकिन बा और बाबू जी ने एक न सुनी.
दूसरी विज़िट में मुझे बाबू जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को और अधिक गहराई से जानने का अवसर मिला. इस बार मैं मिठाई के बजाय, बा और बाबू जी के लिए उपहार ले कर गई. बाबू जी उपहार देख कर मुझे सीख देने पर उतारू हो गए कि बुजुर्गों को भेंट देने की औपचारिकता क्यों की...वगैरा वगैरा....’
पिछले छ: सात माह से फोन और खतों से बातचीत करते-करते और फिर व्यक्तिगत रूप से मिलने पर, मैं भी बाबू जी से काफी परच गई थी. उनकी सीख खत्म होने पर, मैं बड़े इत्मीनान के साथ बोलना शुरू हुई – ‘बाबू जी आप पर आगरा की अलमस्ती तो पूरी तरह पसरी हुई है ही, लेकिन लखनऊ का तकल्लुफी मिजाज भी भरपूर हावी है. ‘बा’ और आप मेरी कितनी आवभगत कर रहे हैं. मैं क्या हूँ आपके लिए - एक शोधार्थी ही तो हूँ. आपसे न खून का रिश्ता है न कोई दूर का. आपका खुले दिल से मेरा इतना सहयोग, स्वागत-सत्कार देखकर मैं कितनी चकित और कृतज्ञ हूँ - मैं बता नहीं सकती. आज के युग में अपने, अपनों को नहीं पूछते और आप दोनों है कि कितना कुछ दिल से कर रहे हैं. ये उपहार मैं नहीं लाई हूँ, बल्कि आप दोनों, जो प्रेम और अपनत्व मुझे दे रहे हैं - वह ‘अपनत्व’ ये भेंट लेकर आया है. तो स्वीकार तो करनी पड़ेगी ‘प्रेम की भेंट’. प्रेम की भेंट तकल्लुफ नहीं होती - यह एक भाग्यशाली का दूसरे भाग्यशाली के साथ भावनात्मक आदान-प्रदान है’.

इसके बाद, दिल से निकली, मेरी इस दलील के आगे दोनों को मेरा उपहार स्वीकार करना पड़ा. उस दूसरी यादगार चर्चा के उपरांत, हम सबने मिलकर भोजन किया. बा के हाथ के स्वादिष्ट व्यंजन और उससे भी अधिक उनकी प्यार भरी भावनाएँ जिनसे खाने का स्वाद और भी दुगुना हो गया था. बाबू जी का चौक का वह घर, आँगन, उनका अध्ययन कक्ष, उनका खडाऊँ पहन कर खटर-पटर करते हुए चलना, पानदान खोल कर पान लगाना और मुँह में गिलौरी रखने का अंदाज़, सरापा प्यार और उदारता से सराबोर व्यक्तित्व, संस्मरण लिखते हुए मेरे ज़ेहन में फिर से जी उठा है.
उन दिनों बाबू जी ‘नाच्यौ बहुत गोपाल’ लिखने में लगे थे. निस्संदेह लेखन कार्य किसी मंथन और तपस्या से कम नहीं होता. कथ्य, भावों और विचारों के पूरी तरह मथे जाने पर ही उत्कृष्ट और कालजयी रचनाएँ निकल कर आती हैं. बाबू जी उपन्यास लेखन से पूर्व, विषय की खूब जांच-पडताल करके, फिर उस पर बाकायदा शोध, छोटी-बड़ी जानकारी, संबंधित सूचनाएँ आदि एक शोधार्थी की भाँति खोजते थे, तदनंतर उस पर कलम चलाते थे. ऎसी सुगढ कृतियों के सृजन के समय - पहले रचनाकार आनंदित होता है और तदनंतर, पठनकाल में, उसे पढने वाले पाठक.

यह मेरा सौभाग्य था कि मैं नागर जी जैसे महान और संवेदनशील रचनाकार से, उनके लेखन के उस दौर में मिली में मिली जब उनका लेखन अपनी पराकाष्ठा पर था. ‘मानस का हंस’ जैसी अमर कृति वे लिख चुके थे और दूसरी कालजयी रचना ‘नाच्यौ बहुत गोपाल’ वे लिख रहे थे. उसके बाद भी १९८१ में ‘खंजन नयन’, १९८२ में ‘बिखरे तिनके’ १९८३ में ‘अग्निगर्भा’, १९८५ में ‘करवट’, और १९८९ में ‘पीढियाँ’ जैसी श्रेष्ठ रचनाएँ उन्होंने साहित्य जगत को दीं. नागर जी की कृतियाँ लंबी उम्र लेकर साहित्य जगत में उतरीं. उनकी रचनाओं के सज्जन-दुर्जन पात्र, अपनी सशक्त चारित्रिक विशेषताओं के साथ पाठकों के दिलों दिमाग पर छा जाने वाले होते थे. मुखर संवेदनाओं का धनी व्यक्ति ही ऐसी, रचनाओं के कथ्य की बुनावट की बारीकियों, पात्रों के अंतर्द्वंद्व से घिरे उनके चरित्रों को ही नहीं वरन मानवीय भावों के पल-पल उलझते-सुलझते तेवरों को समझ सकता था. साथ ही उनकी अभिव्यक्ति, भाषा-शैली इतनी सरल,सहज और तरल कि सीधे दिल में उतरती चली जाए. इन सब खूबियों का समन्वय पहले उनकी रचनाओं में देखने को मिला, तदनंतर मुलाक़ात होने पर उनके व्यक्तित्व में. जिस भावनात्मक ऊष्मा से वे भरपूर थे, वही उष्मा उनके प्रमुख उपन्यास पात्रों में लक्षित हुई मुझे. जब वे बात करते थे, तो शब्दों से ज़्यादा उनके हाव-भाव और चेहरा बोलता था. वे जन्मना साहित्यकार थे. आम ज़िंदगी की अच्छी-बुरी घटनाओं, श्वेत-स्याह चरित्रों को अपने में समोए, उनकी रचनाएँ एक अनूठी ग्राह्यता, और भव्यता ओढ़े होती थीं - ठीक बाबू जी की ही तरह - सरल, सामान्य, फिर भी विशिष्ट और असामान्य.
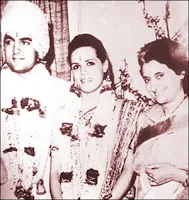 विशेष आलेख:
विशेष आलेख: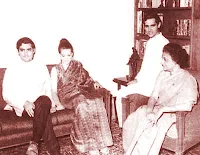
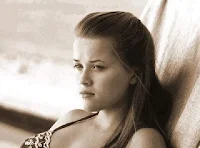 सोनिया के पिता रूसी जेलों में दो साल बिताने के बाद रूस समर्थक हो गये थे। अमेरिकी सेनाओं ने इटली में सभी फासिस्टों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया था। सोनिया ओरबासानो में पैदा नहीं हुईं , जैसा कि सांसद बनने पर उनके द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा में लिखा गया है। उनका जन्म लुसियाना में हुआ था । वह सचयह इसलिए छिपाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके पिता के नाजी और मुसोलिनी संपर्कों का पता न चले साथ ही उनके परिवार के संपर्क इटली के भूमिगत हो चुके नाजी फासिस्टों से द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक बने रहने का सच सबको ज्ञात न हो जाए। लुसियाना इटली-स्विस सीमा पर नाजी फासिस्ट नेटवर्क का मुख्यालय था ।
सोनिया के पिता रूसी जेलों में दो साल बिताने के बाद रूस समर्थक हो गये थे। अमेरिकी सेनाओं ने इटली में सभी फासिस्टों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया था। सोनिया ओरबासानो में पैदा नहीं हुईं , जैसा कि सांसद बनने पर उनके द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा में लिखा गया है। उनका जन्म लुसियाना में हुआ था । वह सचयह इसलिए छिपाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके पिता के नाजी और मुसोलिनी संपर्कों का पता न चले साथ ही उनके परिवार के संपर्क इटली के भूमिगत हो चुके नाजी फासिस्टों से द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक बने रहने का सच सबको ज्ञात न हो जाए। लुसियाना इटली-स्विस सीमा पर नाजी फासिस्ट नेटवर्क का मुख्यालय था । 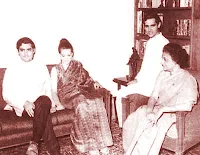
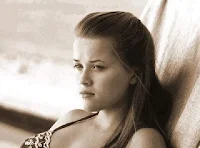 सोनिया के पिता रूसी जेलों में दो साल बिताने के बाद रूस समर्थक हो गये थे। अमेरिकी सेनाओं ने इटली में सभी फासिस्टों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया था। सोनिया ओरबासानो में पैदा नहीं हुईं , जैसा कि सांसद बनने पर उनके द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा में लिखा गया है। उनका जन्म लुसियाना में हुआ था । वह सचयह इसलिए छिपाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके पिता के नाजी और मुसोलिनी संपर्कों का पता न चले साथ ही उनके परिवार के संपर्क इटली के भूमिगत हो चुके नाजी फासिस्टों से द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक बने रहने का सच सबको ज्ञात न हो जाए। लुसियाना इटली-स्विस सीमा पर नाजी फासिस्ट नेटवर्क का मुख्यालय था ।
सोनिया के पिता रूसी जेलों में दो साल बिताने के बाद रूस समर्थक हो गये थे। अमेरिकी सेनाओं ने इटली में सभी फासिस्टों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया था। सोनिया ओरबासानो में पैदा नहीं हुईं , जैसा कि सांसद बनने पर उनके द्वारा प्रस्तुत बायोडाटा में लिखा गया है। उनका जन्म लुसियाना में हुआ था । वह सचयह इसलिए छिपाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके पिता के नाजी और मुसोलिनी संपर्कों का पता न चले साथ ही उनके परिवार के संपर्क इटली के भूमिगत हो चुके नाजी फासिस्टों से द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक बने रहने का सच सबको ज्ञात न हो जाए। लुसियाना इटली-स्विस सीमा पर नाजी फासिस्ट नेटवर्क का मुख्यालय था ।